प्रसंग (Context):
हाल ही में राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत के तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की प्रगति पर सवाल उठाए, खासकर फेज़-2 में कल्पक्कम में तेज़ ब्रीडर रिएक्टर की स्थिति और फेज़-3 के लिए थोरियम रिएक्टरों की योजना को लेकर। यह मुद्दा भारत की दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में उठे कई सवालों को उजागर करता है।
भूमिका और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Background and Origin):
भारत के तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। इसका उद्देश्य भारत को दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रदान करना है, विशेषकर ऐसे देश में जहाँ यूरेनियम सीमित मात्रा में और थोरियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।
तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के चरण (Three Stages):
- प्रथम चरण: प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा संचालित PHWRs (Pressurized Heavy Water Reactors)। इससे प्लूटोनियम उत्पन्न होता है।
- द्वितीय चरण: प्लूटोनियम-आधारित Fast Breeder Reactors (FBRs)। यह U-238 से और अधिक प्लूटोनियम और U-233 उत्पन्न करता है।
- तृतीय चरण: Thorium-232 से U-233 बनाकर बिजली उत्पादन। इसमें Advanced Heavy Water Reactors (AHWR) की भूमिका है।
प्रमुख शब्द और व्याख्या (Key Terms with Notes):
- Plutonium-239: फेज़ 1 से प्राप्त होकर फेज़ 2 में उपयोग होता है।
- Thorium-232: भारत का प्रचुर संसाधन, जिसे U-233 में बदला जाता है।
- Fast Breeder Reactor: उच्च दक्षता और ईंधन उत्पादन क्षमता वाला रिएक्टर।
- AHWR: थोरियम-आधारित अगली पीढ़ी का रिएक्टर।
प्रशासनिक और कानूनी दृष्टिकोण (Administrative and Legal):
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962: सभी परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- DAE & BARC: अनुसंधान और विकास को संचालित करते हैं।
- NPCIL: रिएक्टरों का संचालन करती है।
समाज और पर्यावरणीय दृष्टिकोण (Social & Environmental):
- सुरक्षा और रेडियोधर्मी अपशिष्ट की चिंताएँ
- स्थानीय लोगों की भागीदारी और पुनर्वास
- जैवविविधता और पारिस्थितिकी पर प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण (International Angle):
- 123 समझौता: अमेरिका के साथ परमाणु सहयोग को सक्षम किया।
- NSG: सदस्यता अभी भी लंबित है, तकनीकी बाधा है।
- IAEA निगरानी: कुछ रिएक्टरों को निगरानी में रखा गया है।
चुनौतियाँ (Challenges):
- PFBR निर्माण में देरी
- थोरियम को U-233 में बदलने की जटिलता
- तकनीकी क्षमता और मानव संसाधन की सीमा
हालिया घटनाक्रम (Recent Developments):
- PFBR का 90% निर्माण पूरा, लेकिन कमीशनिंग लंबित
- AHWR डिज़ाइन तैयार, लेकिन निर्माण रुका
- भारत वैश्विक थोरियम अनुसंधान में अग्रणी
UPSC परीक्षा प्रासंगिक बिंदु (UPSC-Relevant Points):
- तीन-स्तरीय योजना की अवधारणा
- भारत का थोरियम भंडार और उपयोग
- PFBR और AHWR का कार्य सिद्धांत
- NSG, IAEA, 123 समझौता
- ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्य और नीति
भारत का तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम
India’s Three-Stage Nuclear Programme
प्रसंग (Context):
हाल ही में राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत के तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की प्रगति पर सवाल उठाए, खासकर फेज़-2 में कल्पक्कम में तेज़ ब्रीडर रिएक्टर की स्थिति और फेज़-3 के लिए थोरियम रिएक्टरों की योजना को लेकर। यह मुद्दा भारत की दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में उठे कई सवालों को उजागर करता है।
भूमिका और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Background and Origin):
भारत के तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। इसका उद्देश्य भारत को दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रदान करना है, विशेषकर ऐसे देश में जहाँ यूरेनियम सीमित मात्रा में और थोरियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।
तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के चरण (Three Stages):
- प्रथम चरण: प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा संचालित PHWRs (Pressurized Heavy Water Reactors)। इससे प्लूटोनियम उत्पन्न होता है।
- द्वितीय चरण: प्लूटोनियम-आधारित Fast Breeder Reactors (FBRs)। यह U-238 से और अधिक प्लूटोनियम और U-233 उत्पन्न करता है।
- तृतीय चरण: Thorium-232 से U-233 बनाकर बिजली उत्पादन। इसमें Advanced Heavy Water Reactors (AHWR) की भूमिका है।
प्रमुख शब्द और व्याख्या (Key Terms with Notes):
- Plutonium-239: फेज़ 1 से प्राप्त होकर फेज़ 2 में उपयोग होता है।
- Thorium-232: भारत का प्रचुर संसाधन, जिसे U-233 में बदला जाता है।
- Fast Breeder Reactor: उच्च दक्षता और ईंधन उत्पादन क्षमता वाला रिएक्टर।
- AHWR: थोरियम-आधारित अगली पीढ़ी का रिएक्टर।
प्रशासनिक और कानूनी दृष्टिकोण (Administrative and Legal):
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962: सभी परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- DAE & BARC: अनुसंधान और विकास को संचालित करते हैं।
- NPCIL: रिएक्टरों का संचालन करती है।
समाज और पर्यावरणीय दृष्टिकोण (Social & Environmental):
- सुरक्षा और रेडियोधर्मी अपशिष्ट की चिंताएँ
- स्थानीय लोगों की भागीदारी और पुनर्वास
- जैवविविधता और पारिस्थितिकी पर प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण (International Angle):
- 123 समझौता: अमेरिका के साथ परमाणु सहयोग को सक्षम किया।
- NSG: सदस्यता अभी भी लंबित है, तकनीकी बाधा है।
- IAEA निगरानी: कुछ रिएक्टरों को निगरानी में रखा गया है।
चुनौतियाँ (Challenges):
- PFBR निर्माण में देरी
- थोरियम को U-233 में बदलने की जटिलता
- तकनीकी क्षमता और मानव संसाधन की सीमा
हालिया घटनाक्रम (Recent Developments):
- PFBR का 90% निर्माण पूरा, लेकिन कमीशनिंग लंबित
- AHWR डिज़ाइन तैयार, लेकिन निर्माण रुका
- भारत वैश्विक थोरियम अनुसंधान में अग्रणी
UPSC परीक्षा प्रासंगिक बिंदु (UPSC-Relevant Points):
- तीन-स्तरीय योजना की अवधारणा
- भारत का थोरियम भंडार और उपयोग
- PFBR और AHWR का कार्य सिद्धांत
- NSG, IAEA, 123 समझौता
- ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्य और नीति
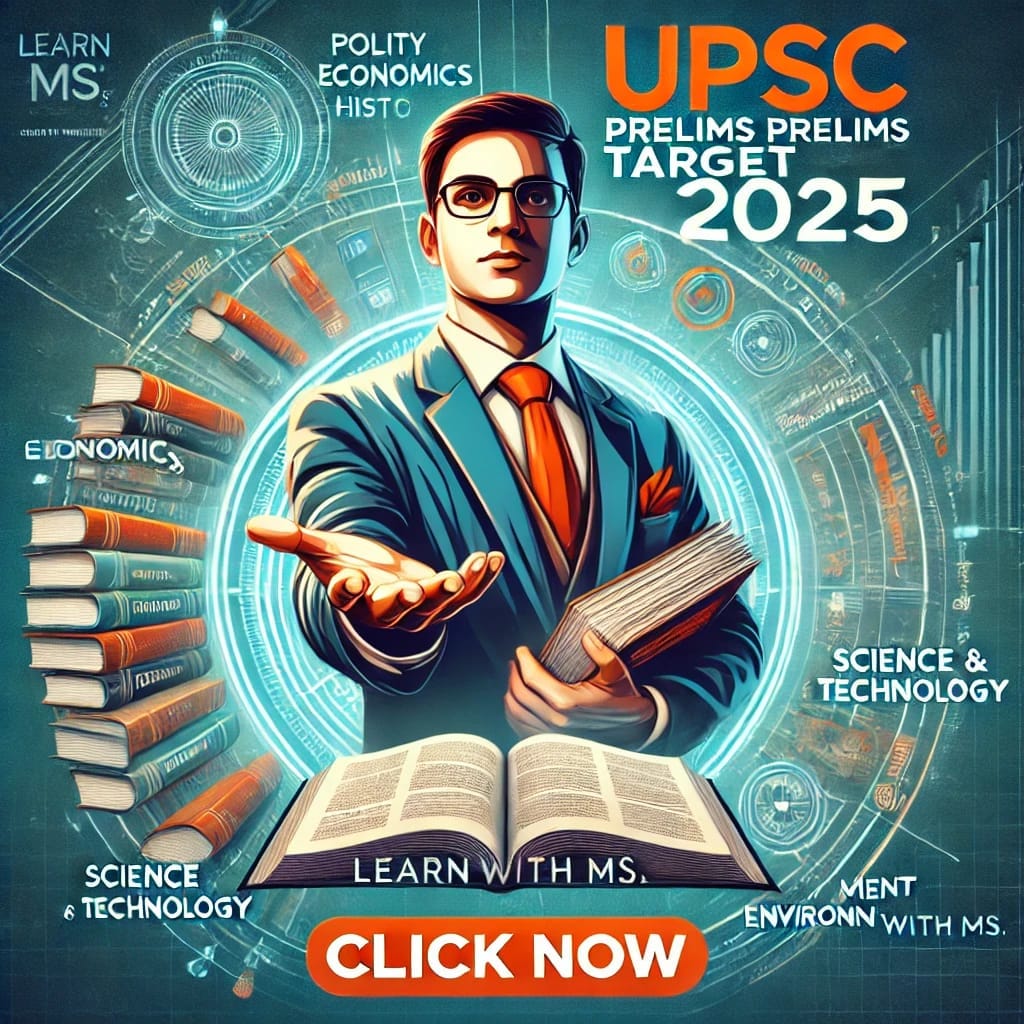
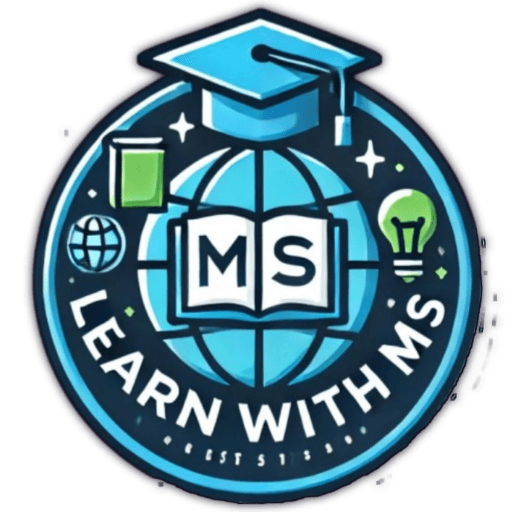
Leave a Reply