DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI FOR UPSC IAS – Prelims And Mains Examination 2025 | 23 JANUARY 2025 – UPSC PRELIMS POINTER Fact Based Current Affairs
DAILY Current Affairs Analysis For UPSC Pre And Mains Examination
Daily Archiveट्रम्प ने जन्म से प्राप्त नागरिकता को समाप्त किया (TRUMP TO END BIRTHRIGHT CITIZENSHIP)
ट्रम्प का जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का प्रस्ताव:
संदर्भ:
हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह प्रस्ताव रखा है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को स्वतः नागरिकता (Birthright Citizenship) का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह कदम अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में बदलाव करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है।
क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship)?
- जन्मसिद्ध नागरिकता का अर्थ है कि कोई भी बच्चा जो अमेरिका की भूमि पर जन्म लेता है, वह स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिक बन जाता है।
- यह अधिकार अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के तहत दिया गया है, जो 1868 में पारित हुआ था।
भारत में नागरिकता
परिचय:
भारत में नागरिकता का विषय संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत संचालित होता है। यह विषय भारतीय राजनीति और सामाजिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह निर्धारित करता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।
भारतीय नागरिकता का संवैधानिक आधार
- संविधान के अनुच्छेद 5-11 (भाग II):
- भारतीय संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है।
- इसमें नागरिकता के लिए बुनियादी प्रावधान दिए गए हैं।
मुख्य अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 5:
भारत के संविधान लागू होने के समय, भारत में जन्मे, भारत में निवास करने वाले, या जिनके माता-पिता भारत में जन्मे हैं, वे नागरिक माने जाएंगे। - अनुच्छेद 6:
भारत विभाजन के बाद, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान। - अनुच्छेद 7:
जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और वापस लौटे, उनके लिए विशेष प्रावधान। - अनुच्छेद 8:
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति (भारतीय वंश) नागरिकता के पात्र हैं। - अनुच्छेद 9:
यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो वह भारतीय नागरिकता का पात्र नहीं होगा। - अनुच्छेद 10:
एक बार नागरिकता मिलने के बाद, इसे कानून के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है। - अनुच्छेद 11:
संसद को नागरिकता के सभी मामलों में कानून बनाने का अधिकार।
नागरिकता प्राप्त करने के तरीके (नागरिकता अधिनियम, 1955):
भारत में नागरिकता पाँच तरीकों से प्राप्त की जा सकती है:
- जन्म के आधार पर (By Birth):
- 1955-1987:
कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, वह नागरिक होगा। - 1987-2004:
कम से कम एक माता-पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक। - 2004 के बाद:
माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
- 1955-1987:
- वंश के आधार पर (By Descent):
- यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है, लेकिन उसके माता-पिता या दादा-दादी भारतीय नागरिक हैं, तो वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
- पंजीकरण के आधार पर (By Registration):
- भारत में रह रहे भारतीय वंश के लोग, जिनकी अन्य देशों में नागरिकता है, पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकते हैं।
- स्वाभाविककरण (By Naturalization):
- वह व्यक्ति जो लगातार 12 साल तक भारत में रह चुका है, और अन्य कानूनी शर्तें पूरी करता है।
- क्षेत्र के विलय के माध्यम से (By Incorporation of Territory):
- भारत के साथ किसी नए क्षेत्र के विलय के बाद वहां के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है।
- उदाहरण: 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के बाद सिक्किमवासियों को नागरिकता दी गई।
नागरिकता समाप्त करने के तरीके:
- त्याग (Renunciation):
- यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है।
- समापन (Termination):
- यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है।
- स्वाभाविककरण रद्द (Deprivation):
- सरकार विशेष परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त कर सकती है, जैसे कि धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA):
मुख्य प्रावधान:
- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान।
- इन प्रवासियों को 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करना आवश्यक है।
- इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया, जिससे यह विवादास्पद बन गया।
विवाद और आलोचना:
- इसे धार्मिक भेदभाव का प्रतीक माना गया।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ मिलाकर इसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खतरा बताया गया।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC):
- परिभाषा:
- NRC एक रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों की सूची बनाई जाती है।
- 2019 में असम में NRC लागू किया गया।
- उद्देश्य:
- अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें बाहर करना।
- चुनौतियाँ:
- लाखों लोगों के दस्तावेजों की कमी के कारण वे सूची में शामिल नहीं हो पाए।
- इसमें सामाजिक और राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए।
भारतीय नागरिकता और वैश्विक तुलना:
| पैरामीटर | भारत | अमेरिका |
|---|---|---|
| जन्मसिद्ध नागरिकता | शर्तों के अधीन। | बिना शर्त। |
| वंश आधारित नागरिकता | उपलब्ध। | सीमित। |
| दोहरे नागरिकता की अनुमति | नहीं। | हाँ। |
| अवैध अप्रवासियों की स्थिति | नागरिकता का कोई अधिकार नहीं। | बच्चों को नागरिकता का अधिकार। |
वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ:
- अवैध प्रवासी:
- बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों से आए अप्रवासियों की पहचान और समाधान।
- भारत में अनुमानित 2 करोड़ से अधिक अवैध प्रवासी हो सकते हैं।
- CAA और NRC का विरोध:
- इन नीतियों को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताते हुए व्यापक प्रदर्शन हुए।
- सरकार ने इन्हें भारत की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया।
- दोहरी नागरिकता का अभाव:
- कई भारतीय जो अन्य देशों में बस गए हैं, वे दोहरी नागरिकता की मांग कर रहे हैं।
- वर्तमान में, प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) का दर्जा दिया जाता है, जो सीमित अधिकार प्रदान करता है।
आगे की राह:
- संतुलित नीति निर्माण:
- नागरिकता कानूनों को समानता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित करना।
- अवैध प्रवासियों की समस्या का समाधान:
- स्पष्ट और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना।
- दोहरी नागरिकता:
- भारत को दोहरी नागरिकता के प्रावधान पर विचार करना चाहिए।
निष्कर्ष:
भारत में नागरिकता का विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक एकता और मानवाधिकारों के संतुलन से जुड़ा हुआ है।
नागरिकता से संबंधित कानूनों को संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ लागू करना आवश्यक है, ताकि भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।
डोनाल्ड ट्रम्प का प्रस्ताव
- प्रस्ताव का उद्देश्य:
- अवैध प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता देने की प्रक्रिया पर रोक लगाना।
- ट्रम्प का तर्क है कि यह नीति अप्रवासियों को अमेरिका में आने के लिए प्रेरित करती है।
- संभावित कार्यप्रणाली:
- ट्रम्प ने घोषणा की है कि वे यह बदलाव एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) के माध्यम से लागू करना चाहेंगे।
- यह आदेश उन बच्चों को नागरिकता से वंचित कर देगा जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी प्रवासी नहीं हैं।
संवैधानिक और कानूनी प्रश्न
- संविधान का 14वां संशोधन:
- यह संशोधन कहता है:
“सभी व्यक्ति जो अमेरिका में जन्मे हैं या प्राकृतिक रूप से अमेरिका में नागरिक बने हैं, वे अमेरिका के नागरिक हैं।” - इस संशोधन में बदलाव करना कठिन है क्योंकि इसके लिए कांग्रेस और राज्यों की सहमति आवश्यक होगी।
- यह संशोधन कहता है:
- संवैधानिक विवाद:
- ट्रम्प का प्रस्ताव कानूनी लड़ाई का कारण बन सकता है क्योंकि यह संशोधन सीधे अमेरिकी मूल अधिकारों से संबंधित है।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि एक कार्यकारी आदेश संविधान को ओवरराइड नहीं कर सकता।
समाज और राजनीति पर प्रभाव
- प्रवासी समुदाय पर प्रभाव:
- लाखों अप्रवासी परिवार प्रभावित हो सकते हैं।
- यह नीति अमेरिका के अप्रवासी समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकती है।
- राजनीतिक ध्रुवीकरण:
- ट्रम्प का यह कदम उनके समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कदम के रूप में देख सकते हैं।
- इससे अमेरिका की राजनीति में नस्ल और प्रवास के मुद्दे पर और अधिक ध्रुवीकरण हो सकता है।
विपक्ष और समर्थन
- समर्थन:
- ट्रम्प के समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक मानते हैं।
- वे इसे गैर-कानूनी प्रवासियों को रोकने का प्रभावी तरीका मानते हैं।
- विपक्ष:
- मानवाधिकार कार्यकर्ता और डेमोक्रेटिक पार्टी इसे असंवैधानिक और विभाजनकारी कदम मानते हैं।
- यह अमेरिकी समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
- जन्मसिद्ध नागरिकता केवल कुछ देशों में मान्य है, जैसे:
- अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील।
- यदि अमेरिका इस नीति को बदलता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय अप्रवासी नीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
आगे की राह
- कानूनी प्रक्रिया:
- इस प्रस्ताव पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी जा सकती है।
- इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
- नीति में संतुलन:
- यह जरूरी है कि अप्रवासी नीतियों और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाया जाए।
- अप्रवासी समुदायों के योगदान को ध्यान में रखते हुए समावेशी नीति बनानी चाहिए।
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्प का जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने का प्रस्ताव अमेरिका के राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह न केवल संविधान के मूल अधिकारों को चुनौती देता है, बल्कि वैश्विक अप्रवासी नीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
इस प्रस्ताव को लागू करने में कानूनी और राजनीतिक बाधाएं होंगी, लेकिन यह अमेरिका में अप्रवासी नीतियों के प्रति दृष्टिकोण को नया आयाम दे सकता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती – “पराक्रम दिवस”
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती – “पराक्रम दिवस”
संदर्भ
- 2021 से हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को “पराक्रम दिवस” या वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 2025 में नेताजी की 128वीं जयंती मनाई जा रही है।
- इस दिवस को स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान को सम्मानित करने और उनके अदम्य साहस को याद करने के लिए घोषित किया गया।
नेताजी का जीवन परिचय
- जन्म:
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ।
- वे एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की।
- स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष (1938-1939)।
- उन्होंने गांधीजी के अहिंसात्मक दृष्टिकोण के विपरीत एक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया।
- फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज (INA) की स्थापना की।
- उनका प्रसिद्ध नारा था: “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।”
पराक्रम दिवस का महत्त्व
- राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत:
- यह दिन नेताजी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, वीरता और नेतृत्व क्षमता को सम्मानित करता है।
- देश के युवाओं के लिए प्रेरणा:
- नेताजी का जीवन युवाओं को कठिन परिस्थितियों में भी निडरता और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना सिखाता है।
- भारतीय सेना में प्रेरणा का स्रोत:
- आजाद हिंद फौज ने भारतीय सेना को अनुशासन, साहस और बलिदान का पाठ सिखाया।
पराक्रम दिवस 2025 के विशेष कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कार्यक्रम:
- नई दिल्ली में “नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक” पर पुष्पांजलि अर्पित।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शनी।
- स्कूलों और कॉलेजों में आयोजन:
- निबंध प्रतियोगिताएँ और भाषण।
- नेताजी के जीवन पर फिल्में और नाटकों का प्रदर्शन।
- प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान:
- नेताजी से संबंधित संग्रहालयों और स्मारकों में विशेष प्रदर्शनी।
नेताजी की शिक्षाएँ और आज का भारत
- स्वराज का सपना:
- नेताजी ने पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की कल्पना की थी।
- आज भारत आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भरता) के विचार को बढ़ावा दे रहा है।
- संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा:
- उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत करने की नींव रखी।
- आज भारतीय सेना वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति बन चुकी है।
- एकता का संदेश:
- नेताजी का मानना था कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है।
- उनके आदर्श “जय हिंद” ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बाँधा।
आगे की राह
- नेताजी के विचारों और आदर्शों को शिक्षा और पाठ्यक्रम में शामिल करना।
- भारत के युवाओं में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का भाव जगाना।
- नेताजी से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और प्रचार।
निष्कर्ष
नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय नायक थे। उनकी जयंती को “पराक्रम दिवस” के रूप में मनाना न केवल उनके साहस और बलिदान को सम्मानित करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा देने का भी एक प्रयास है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के संबंध
नेताजी और गांधीजी का परस्पर दृष्टिकोण
महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख स्तंभ थे। हालांकि, दोनों के उद्देश्य समान थे—भारत को स्वतंत्र कराना—लेकिन उनके विचार और कार्य करने के तरीके अलग-अलग थे।
संबंधों का विकास और तनाव
- शुरुआती समर्थन:
- नेताजी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती चरणों में सराहा।
- उन्होंने गांधीजी को “राष्ट्रपिता” कहा और उनके अहिंसात्मक आंदोलन को प्रेरणा मानते हुए कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई।
- विचारधारा का टकराव:
- गांधीजी अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करते थे, जबकि नेताजी सशस्त्र संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय समर्थन की वकालत करते थे।
- नेताजी मानते थे कि ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए बल का उपयोग अनिवार्य है।
- कांग्रेस अध्यक्ष पद का विवाद (1939):
- नेताजी ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा।
- गांधीजी ने पट्टाभि सीतारमैया का समर्थन किया, लेकिन नेताजी ने यह चुनाव जीत लिया।
- हालांकि, उनके और गांधीजी के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण नेताजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
नेताजी का अलग रास्ता
- गांधीजी के शांतिपूर्ण आंदोलन के विपरीत, नेताजी ने आजाद हिंद फौज (INA) का गठन किया और विदेशी सहयोग (जर्मनी और जापान) के माध्यम से भारत को आजादी दिलाने का प्रयास किया।
- इसके बावजूद, नेताजी ने गांधीजी को “महात्मा” मानकर हमेशा उनका सम्मान किया।
परस्पर सम्मान
- नेताजी का गांधीजी के प्रति सम्मान:
- 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो पर अपने प्रसिद्ध संबोधन में नेताजी ने गांधीजी को “राष्ट्रपिता” कहकर संबोधित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा।
- यह संबोधन दर्शाता है कि मतभेदों के बावजूद नेताजी के मन में गांधीजी के प्रति गहरा सम्मान था।
- गांधीजी का नेताजी के प्रति दृष्टिकोण:
- गांधीजी ने नेताजी के संघर्ष और बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन हिंसा के मार्ग को सही नहीं ठहराया।
- नेताजी के निधन पर गांधीजी ने कहा, “नेताजी की मृत्यु ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी है।”
दो दृष्टिकोणों की भूमिका
- गांधीजी और नेताजी दोनों का दृष्टिकोण भारत की स्वतंत्रता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था।
- गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदल दिया, जबकि नेताजी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के संघर्ष को पहचान दिलाई।
- एक तरफ गांधीजी का सत्य और अहिंसा का मार्ग था, तो दूसरी तरफ नेताजी का साहस और बलिदान।
निष्कर्ष
महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों के बावजूद, दोनों के उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे। उनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जटिलता और विविधता को दर्शाता है।
नेताजी और गांधीजी के विचार हमें यह सिखाते हैं कि एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भिन्न दृष्टिकोण भी सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना और सुकन्या समृद्धि योजना
Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) Scheme and Sukanya Samriddhi Yojana
चर्चा में क्यों?
22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के शुभारंभ का 10वाँ वर्ष मनाया गया। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य भारत में बालिकाओं के जीवन, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण में इन योजनाओं के योगदान की समीक्षा की।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना:
परिचय
- शुभारंभ: 22 जनवरी 2015।
- उद्देश्य:
- लैंगिक अनुपात में सुधार करना।
- बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना।
- जागरूकता फैलाना और लैंगिक भेदभाव कम करना।
- संयुक्त प्रयास: यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) का संयुक्त कार्यक्रम है।
मुख्य घटक:
- जागरूकता:
- समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
- सेवा वितरण:
- स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- लैंगिक अनुपात में सुधार:
- बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio – CSR) को सुधारना।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): परिचय
- शुभारंभ: 22 जनवरी 2015।
- उद्देश्य:
- बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा।
- शिक्षा और शादी के लिए बचत को प्रोत्साहन।
- विशेषताएँ:
- किसी भी बालिका के नाम पर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है।
- प्रारंभिक निवेश ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष।
- आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ।
- मैच्योरिटी अवधि: 21 वर्ष या बालिका की शादी।
भारत में लैंगिक संकेतकों में प्रगति (2015-2025)
1. बाल लिंगानुपात (CSR):
- 2015 में: 918 लड़कियाँ प्रति 1,000 लड़कों।
- 2025 में: 934 लड़कियाँ प्रति 1,000 लड़कों।
- सुधार के कारण: जागरूकता अभियानों और अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग पर सख्त निगरानी।
2. महिला साक्षरता दर:
- 2015 में: 65.5%।
- 2025 में: 71.2%।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे BBBP और SSA (सर्व शिक्षा अभियान) के माध्यम से वृद्धि।
3. मातृ मृत्यु दर (MMR):
- 2015 में: प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 167।
- 2025 में: प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 103।
- सुरक्षित प्रसव और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
4. महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर (LFPR):
- 2015 में: 23%।
- 2025 में: 28%।
- योजनाओं और महिला कौशल विकास कार्यक्रमों ने इसे बढ़ावा दिया।
5. बालिकाओं के स्कूल नामांकन:
- 2015 में: 92%।
- 2025 में: 98.5%।
- स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार और छात्रवृत्ति योजनाएँ प्रभावी रहीं।
चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता
चुनौतियाँ:
- गहरी सामाजिक बंधन:
- बालिकाओं के प्रति अभी भी कई क्षेत्रों में नकारात्मक सोच।
- पितृसत्तात्मक संरचना के कारण योजनाओं का सीमित प्रभाव।
- लिंग आधारित भेदभाव:
- उच्च शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी कम।
- कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव।
- सामाजिक सुरक्षा का अभाव:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजनाओं का असमान कार्यान्वयन।
आगे की राह:
- जागरूकता अभियानों को मजबूत करना:
- स्थानीय भाषाओं और माध्यमों में प्रभावी जागरूकता अभियान।
- धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों की भागीदारी।
- कार्यस्थल पर समानता:
- महिलाओं के लिए समान वेतन और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश:
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
- समीक्षा और निगरानी:
- योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा।
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।
- सामाजिक सुरक्षा का विस्तार:
- बालिकाओं के लिए विशेष बीमा योजनाएँ।
- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता।
निष्कर्ष:
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना ने पिछले एक दशक में बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इन योजनाओं के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक बदलाव के माध्यम से भारत लैंगिक समानता के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
UPSC दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न
प्रीलिम्स:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ था?
- उत्तर: 22 जनवरी 2015।
- सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी अवधि कितनी है?
- उत्तर: 21 वर्ष।
- भारत में 2025 तक बाल लिंगानुपात क्या है?
- उत्तर: 934 लड़कियाँ प्रति 1,000 लड़कों।
मुख्य परीक्षा:
- प्रश्न: “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना की सफलता और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।”
- प्रश्न: “सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करें।”
- प्रश्न: “भारत में बालिकाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रभाव का आकलन कीजिए।”
वृद्धजनों की समस्या से संबंधित मामला ( matter related to the problems of the elderly )
चर्चा में क्यों?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वृद्धजनों के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि देश में वृद्धजनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उनके कल्याण के लिए समर्पित मंत्रालय की आवश्यकता है। हालांकि, न्यायालय ने यह कहा कि इस विषय पर निर्णय लेना विधायिका का कार्यक्षेत्र है और उसने याचिका खारिज कर दी।
वृद्धजन: परिभाषा और स्थिति
- परिभाषा: आमतौर पर, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धजन माना जाता है।
- भारत में वृद्धजनों की स्थिति:
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में वृद्धजनों की संख्या लगभग 10.38 करोड़ थी।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट (2021) के अनुसार, 2050 तक यह संख्या 20% से अधिक होने की संभावना है।
- स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन वृद्धजनों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
रिट याचिका: परिचय और प्रासंगिकता
रिट याचिका (Writ Petition):
- संविधान के अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट के लिए) और अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट के लिए) के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका दायर की जा सकती है।
- प्रमुख प्रकार: हबेअस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, और क्वो वारंटो।
याचिका में मुख्य मांगें:
- वृद्धजनों के लिए समर्पित मंत्रालय:
- वृद्धजनों की समस्याओं को हल करने के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना।
- कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी:
- मौजूदा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और नई योजनाएँ बनाने के लिए समर्पित प्राधिकरण।
सुप्रीम कोर्ट का उत्तर:
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन का निर्णय संसद या कार्यपालिका का काम है।

भारत में वृद्धजनों की स्थिति:
भारत में वृद्धजनों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों) की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव देश की जनसांख्यिकीय संरचना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, और पारिवारिक संरचना में हो रहे बदलावों का परिणाम है। वृद्धजनों की बढ़ती आबादी सामाजिक, आर्थिक, और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को जन्म दे रही है।
प्रमुख आंकड़े और तथ्य
- जनसंख्या:
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 10.38 करोड़ थी।
- NSO की रिपोर्ट (2021): यह संख्या 2050 तक कुल जनसंख्या का 20% होने की संभावना है।
- जीवन प्रत्याशा:
- स्वतंत्रता के बाद, जीवन प्रत्याशा 37 वर्ष थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 वर्ष हो गई है।
- लैंगिक अनुपात:
- वृद्ध महिलाओं की संख्या वृद्ध पुरुषों की तुलना में अधिक है, लेकिन वे अधिकतर आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक कमजोर हैं।
वृद्धजनों की समस्याएँ
1. आर्थिक समस्याएँ:
- आय का अभाव:
- 70% से अधिक वृद्धजन असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, जहाँ पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।
- निर्भरता:
- अधिकतर वृद्धजन अपने बच्चों या परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं।
- पेंशन की समस्या:
- सीमित पेंशन योजनाएँ और कम कवरेज।
2. स्वास्थ्य समस्याएँ:
- बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल की कमी:
- भारत में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ अपर्याप्त हैं।
- गैर-संचारी रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, और कैंसर आम हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य:
- अकेलापन, डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी मानसिक समस्याएँ।
- दीर्घकालिक देखभाल:
- दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं और नर्सिंग होम की कमी।
3. सामाजिक समस्याएँ:
- अकेलापन और उपेक्षा:
- पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन।
- शहरीकरण के कारण बच्चे वृद्धजनों से दूर रहने लगे हैं।
- बुजुर्गों के प्रति असंवेदनशीलता:
- बुजुर्गों को समाज में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमतर माना जाता है।
- दुर्व्यवहार:
- 2019 के एक अध्ययन के अनुसार, 40% वृद्धजन घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करते हैं।
4. कानूनी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव:
- वृद्धजनों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत ढाँचे का अभाव।
भारत में वृद्धजनों के लिए मौजूदा कानून और योजनाएँ
1. कानूनी प्रावधान:
- अनुवृत्ति और कल्याण अधिनियम, 2007 (MWPSC):
- बच्चों और रिश्तेदारों को माता-पिता और वृद्धजनों की देखभाल के लिए कानूनी बाध्यता।
- माता-पिता को भरण-पोषण के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करने का अधिकार।
- भारतीय दंड संहिता (IPC):
- धारा 125 के तहत, माता-पिता अपने बच्चों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
2. योजनाएँ:
- राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य कार्यक्रम (NPHCE):
- वृद्धजनों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ।
- अटल पेंशन योजना (APY):
- वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करना।
- वृद्धजन हेल्पलाइन (14567):
- वृद्धजनों को समर्थन और सहायता।
वृद्धजनों के लिए मंत्रालय की आवश्यकता का विश्लेषण
तर्क में समर्थन:
- विशेष ध्यान:
- वृद्धजनों की समस्याएँ (स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक अलगाव) विशिष्ट हैं और एक समर्पित मंत्रालय इन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकता है।
- कार्यक्रमों का समन्वय:
- वृद्धजनों के लिए कई योजनाएँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन में कमी है।
- भविष्य की तैयारी:
- भारत में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है।
तर्क में विरोध:
- प्रभावी उपयोग की आवश्यकता:
- मौजूदा योजनाओं और संस्थानों के बेहतर कार्यान्वयन से वृद्धजनों की समस्याएँ हल की जा सकती हैं।
- संसाधनों की सीमितता:
- नया मंत्रालय स्थापित करने से प्रशासनिक लागत बढ़ सकती है।
- संवैधानिक सीमाएँ:
- सरकार के प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन का निर्णय कार्यपालिका और विधायिका का क्षेत्र है।
समाधान और सुझाव
- मौजूदा ढाँचे को सुदृढ़ करना:
- मौजूदा योजनाओं और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- राज्य और जिला स्तर पर वृद्धजन सहायता केंद्रों की स्थापना।
- समर्पित प्राधिकरण:
- वृद्धजनों के कल्याण के लिए एक केंद्रीय एजेंसी का गठन जो मौजूदा योजनाओं का समन्वय और निगरानी करे।
- आर्थिक सुरक्षा:
- वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार।
- पेंशन योजनाओं में सुधार और उनकी पहुंच बढ़ाना।
- सामाजिक समावेशन:
- परिवार और समुदाय स्तर पर वृद्धजनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना।
- वृद्धजनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- शोध और डाटा संग्रहण:
- वृद्धजनों से संबंधित डेटा का संग्रहण और विश्लेषण।
- भविष्य की नीतियों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
निष्कर्ष:
भारत में वृद्धजनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और उनके कल्याण के लिए सुदृढ़ योजनाओं और नीतियों की आवश्यकता है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने समर्पित मंत्रालय की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन यह विषय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ है। वृद्धजनों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार, समाज और समुदाय को मिलकर कार्य करना होगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WORLD HEALTH ORGANIZATION)
प्रसंग
संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकल जाएगा। यह कदम उन्होंने COVID-19 महामारी और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में WHO की कथित विफलताओं के कारण उठाया। यह निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक बड़ा झटका था और इसका व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव पड़ा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO): परिचय
- स्थापना: 7 अप्रैल 1948।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- कार्य:
- वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व करना।
- स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।
- महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सहयोग और सहायता प्रदान करना।
डोनाल्ड ट्रम्प के आरोप और तर्क
- COVID-19 प्रबंधन में विफलता:
- ट्रम्प ने WHO पर चीन के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया।
- उन्होंने कहा कि WHO ने महामारी की शुरुआत में पारदर्शिता नहीं रखी और समय पर चेतावनी देने में विफल रहा।
- चीन के प्रभाव का मुद्दा:
- ट्रम्प के अनुसार, WHO ने COVID-19 महामारी की गंभीरता को छिपाने में चीन की सहायता की।
- यह भी आरोप लगाया गया कि WHO ने महामारी की उत्पत्ति की निष्पक्ष जांच नहीं की।
- अमेरिकी वित्तीय योगदान:
- अमेरिका WHO का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता था।
- ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका WHO को हर साल लगभग 400 मिलियन डॉलर देता है, लेकिन इसे उचित प्रतिनिधित्व या पारदर्शिता नहीं मिलती।
वैश्विक प्रभाव
- स्वास्थ्य प्रयासों पर प्रभाव:
- WHO को अमेरिकी धन का बड़ा हिस्सा मिलता था, जिसका उपयोग टीकाकरण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य अनुसंधान और महामारी प्रबंधन में किया जाता था।
- अमेरिका के बाहर निकलने से WHO के इन कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रभाव:
- WHO वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के दौरान देशों के बीच समन्वय करने वाली प्रमुख संस्था है।
- अमेरिका के बाहर निकलने से वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में विभाजन का खतरा बढ़ गया।
- चीन की भूमिका का विस्तार:
- अमेरिका के कदम के बाद, चीन ने WHO में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया।
- चीन ने WHO को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
समाधान और सुझाव
- वैश्विक स्वास्थ्य सुधार:
- WHO को अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।
- सदस्य देशों के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
- स्वतंत्र जांच:
- वैश्विक स्वास्थ्य संकटों की उत्पत्ति और प्रबंधन पर स्वतंत्र जांच के लिए तंत्र विकसित किए जाएं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
- सदस्य देशों को अपने मतभेदों को सुलझाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।
- वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग बढ़ाया जाए।
- स्वास्थ्य वित्तपोषण:
- WHO को वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए।
- महामारी के दौरान वित्तीय संकट से बचने के लिए आपातकालीन कोष की स्थापना।
निष्कर्ष:
अमेरिका का WHO से बाहर निकलना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जिसने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया। COVID-19 महामारी जैसी आपदाएँ यह साबित करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना और सदस्य देशों का सहयोग बढ़ाना अनिवार्य है। WHO को अपनी कमियों को दूर कर एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के रूप में उभरने की दिशा में काम करना चाहिए।
UPSC दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न
प्रीलिम्स संभावित प्रश्न
- विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
- उत्तर: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं (2025 तक)?
- उत्तर: टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस।
- WHO का गठन किस वर्ष हुआ था?
- उत्तर: 1948।
मुख्य परीक्षा संभावित प्रश्न
- प्रश्न: COVID-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का विश्लेषण करें।
- प्रश्न: अमेरिका के WHO से बाहर निकलने का वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा?
- प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सदस्य देशों के वित्तीय योगदान और पारदर्शिता के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए।
बोरियल वन (BOREAL FORESTS) – Upsc prelims pointer
प्रसंग
एक नए अध्ययन के अनुसार, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया में फैले बोरियल वनों का लगभग आधा हिस्सा जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े बदलावों का सामना कर रहा है। इन बदलावों से ये वन जंगल की आग के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं और वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका खतरे में पड़ गई है। यह स्थिति न केवल पर्यावरणीय संतुलन बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है।
बोरियल वन: परिचय
- स्थान: बोरियल वन, जिन्हें टैगा भी कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में कनाडा, अलास्का, रूस (साइबेरिया), और स्कैंडिनेविया जैसे ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- प्रमुख विशेषता:
- ये वन पृथ्वी की सतह का लगभग 17% भाग कवर करते हैं।
- मुख्य रूप से शंकुधारी पेड़, जैसे स्प्रूस, पाइन और फर के लिए प्रसिद्ध हैं।
- भूमिका:
- कार्बन सिंक: ये वन वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं।
- प्राकृतिक संतुलन: जैव विविधता का समर्थन और जलवायु को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण।
अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:
- बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघल रही है और मिट्टी की नमी कम हो रही है।
- लंबे और शुष्क गर्मी के मौसम के कारण जंगल की आग की घटनाएं बढ़ रही हैं।
- जंगल की आग का खतरा:
- बोरियल वनों में आग लगने की घटनाएं पहले से अधिक तीव्र और व्यापक हो गई हैं।
- आग के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जारी हो रहा है, जिससे जलवायु संकट और गहरा रहा है।
- कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत:
- वनों की आग और बढ़ते अपघटन के कारण बोरियल वन कार्बन अवशोषित करने के बजाय उत्सर्जन का स्रोत बन सकते हैं।
- जैव विविधता पर प्रभाव:
- तापमान में वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो रहे हैं।
- वन्यजीवों की आदतें और प्रजातियों का वितरण प्रभावित हो रहा है।
बोरियल वनों के महत्व और संकट
महत्व:
- कार्बन अवशोषण: बोरियल वन वैश्विक कार्बन चक्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं का नियंत्रण: ये वन जलवायु को स्थिर रखते हैं और बाढ़ व सूखे जैसी आपदाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- जैव विविधता का संरक्षण: ये वन सैकड़ों प्रजातियों का घर हैं, जिनमें कई संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं।
संकट:
- जंगल की आग में वृद्धि: उच्च तापमान और शुष्क मौसम के कारण आग की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है।
- पर्यावरणीय असंतुलन: मिट्टी का क्षरण, जलवायु प्रणाली का असंतुलन और वन्यजीवों का निवास स्थान प्रभावित हो रहा है।
- मानव जीवन पर प्रभाव: इन वनों की बिगड़ती स्थिति से स्थानीय समुदायों और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयासों पर असर पड़ रहा है।
समाधान और नीति सुझाव
1. जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण:
- ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।
2. आग प्रबंधन:
- जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना।
- आग प्रतिरोधी प्रबंधन तकनीकों का उपयोग।
3. जैव विविधता संरक्षण:
- वन्यजीव आवासों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण कार्यक्रम।
- प्रजातियों के वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों पर शोध।
4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग:
- जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग।
- विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता।
5. स्थानीय समुदायों की भागीदारी:
- वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।
- पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के समन्वय से समाधान।
निष्कर्ष:
बोरियल वनों का जलवायु परिवर्तन के कारण संकटग्रस्त होना एक वैश्विक चेतावनी है। ये वन न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अनमोल हैं। इनकी सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास, टिकाऊ नीतियाँ और सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। बोरियल वनों की स्थिति को सुधारना केवल एक पर्यावरणीय कदम नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी है।
UPSC दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न
1. प्रीलिम्स के लिए संभावित प्रश्न:
- बोरियल वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
- उत्तर: उत्तरी गोलार्ध (कनाडा, अलास्का, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया)।
- टैगा वन का मुख्य वृक्ष कौन सा है?
- उत्तर: शंकुधारी वृक्ष जैसे स्प्रूस, पाइन, और फर।
- बोरियल वनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है?
- उत्तर: कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना।
2. मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:
- प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के कारण बोरियल वनों की बिगड़ती स्थिति का पर्यावरणीय प्रभावों के साथ विश्लेषण कीजिए।
- प्रश्न: बोरियल वनों के संकट को देखते हुए वैश्विक कार्बन सिंक के प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम सुझाइए।
- प्रश्न: जंगल की आग के कारण पर्यावरण और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कीजिए।
इंडोनेशिया का माउंट इबू में भूगर्भिक गतिविधि ( Geological activity at Mount Ibu in Indonesia )
प्रसंग
इंडोनेशिया का माउंट इबू इस महीने कम से कम 1,000 बार फट चुका है। यह घटनाक्रम क्षेत्रीय भूगर्भीय गतिविधियों में वृद्धि का संकेत है। इस दौरान हजारों ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी हैं। माउंट इबू की इस सक्रियता ने न केवल स्थानीय क्षेत्र बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है।
माउंट इबू के बारे में जानकारी
- स्थान: माउंट इबू इंडोनेशिया के मालुकु द्वीप समूह (Halmahera Island) पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
- ऊंचाई: लगभग 1,325 मीटर।
- प्रमुख विशेषता: यह एक स्ट्रेटोवोल्कैनो (Stratovolcano) है, जो परतों में लावा, राख और पिघले हुए पत्थरों के जमाव से बना होता है।
- हाल की गतिविधि: माउंट इबू पिछले कई वर्षों से सक्रिय है और समय-समय पर विस्फोट करता रहा है।
ज्वालामुखी विस्फोट के कारण और प्रभाव
कारण:
- ज्वालामुखीय गतिविधि:
- इंडोनेशिया “रिंग ऑफ फायर” का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र है।
- प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण उप-डक्शन ज़ोन (Subduction Zones) में ज्वालामुखीय विस्फोट होते हैं।
- भूगर्भीय अस्थिरता:
- इंडोनेशिया में प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट का आपस में टकराव।
- इस प्रक्रिया के दौरान मैग्मा सतह पर आ जाता है।
प्रभाव:
- स्थानीय प्रभाव:
- जीवन और संपत्ति का नुकसान: विस्फोट के कारण राख और लावा के प्रवाह से लोगों की जान-माल को खतरा।
- स्वास्थ्य प्रभाव: ज्वालामुखीय राख में मौजूद गैसें (जैसे सल्फर डाइऑक्साइड) श्वसन समस्याएं पैदा कर सकती हैं।
- आर्थिक नुकसान: कृषि और स्थानीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव।
- वैश्विक प्रभाव:
- वायुमंडलीय प्रभाव: राख और गैसें वायुमंडल में पहुंचकर वैश्विक तापमान को प्रभावित कर सकती हैं।
- पर्यावरणीय नुकसान: विस्फोट से आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
राहत और बचाव कार्य
- निकासी:
- ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है।
- मॉनिटरिंग सिस्टम:
- इंडोनेशिया की ज्वालामुखी और भूभौतिकी एजेंसी (PVMBG) द्वारा विस्फोट की निगरानी।
- चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
- अन्य देशों और संस्थाओं से सहायता।
- वैज्ञानिक अध्ययन और वैश्विक सतर्कता।
समाधान और नीति सुझाव
- आपदा प्रबंधन में सुधार:
- बेहतर चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन तंत्र।
- निकासी योजनाओं को सुदृढ़ करना।
- वैश्विक सहयोग:
- ज्वालामुखी गतिविधियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान।
- संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग।
- शिक्षा और जागरूकता:
- स्थानीय समुदायों को आपदा से संबंधित जागरूकता प्रदान करना।
- बचाव और राहत कार्यों में नागरिक भागीदारी।
- तकनीकी निवेश:
- सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम।
- ज्वालामुखी पूर्वानुमान मॉडल का विकास।
निष्कर्ष:
माउंट इबू की सक्रियता इंडोनेशिया और वैश्विक पर्यावरणीय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह घटना न केवल प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी तैयारियों को जांचती है, बल्कि वैश्विक सहयोग और तकनीकी निवेश की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। ज्वालामुखीय गतिविधियों से निपटने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
UPSC के दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न
1. प्रीलिम्स के लिए संभावित प्रश्न
- माउंट इबू किस देश में स्थित है?
- उत्तर: इंडोनेशिया।
- “रिंग ऑफ फायर” का क्या अर्थ है?
- उत्तर: प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र।
- स्ट्रेटोवोल्कैनो क्या है?
- उत्तर: एक प्रकार का ज्वालामुखी जो परतों में लावा, राख और अन्य पदार्थों से बना होता है।
- इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधि क्यों होती है?
- उत्तर: यह क्षेत्र प्रशांत, यूरेशियन और इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उप-डक्शन ज़ोन पर स्थित है।
2. मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
- प्रश्न: ज्वालामुखी विस्फोट के वैश्विक पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का आकलन कीजिए।
- प्रश्न: आपदा प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीक की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- प्रश्न: “रिंग ऑफ फायर” की भूमिका के संदर्भ में इंडोनेशिया की भूगर्भीय सक्रियता का विश्लेषण कीजिए।
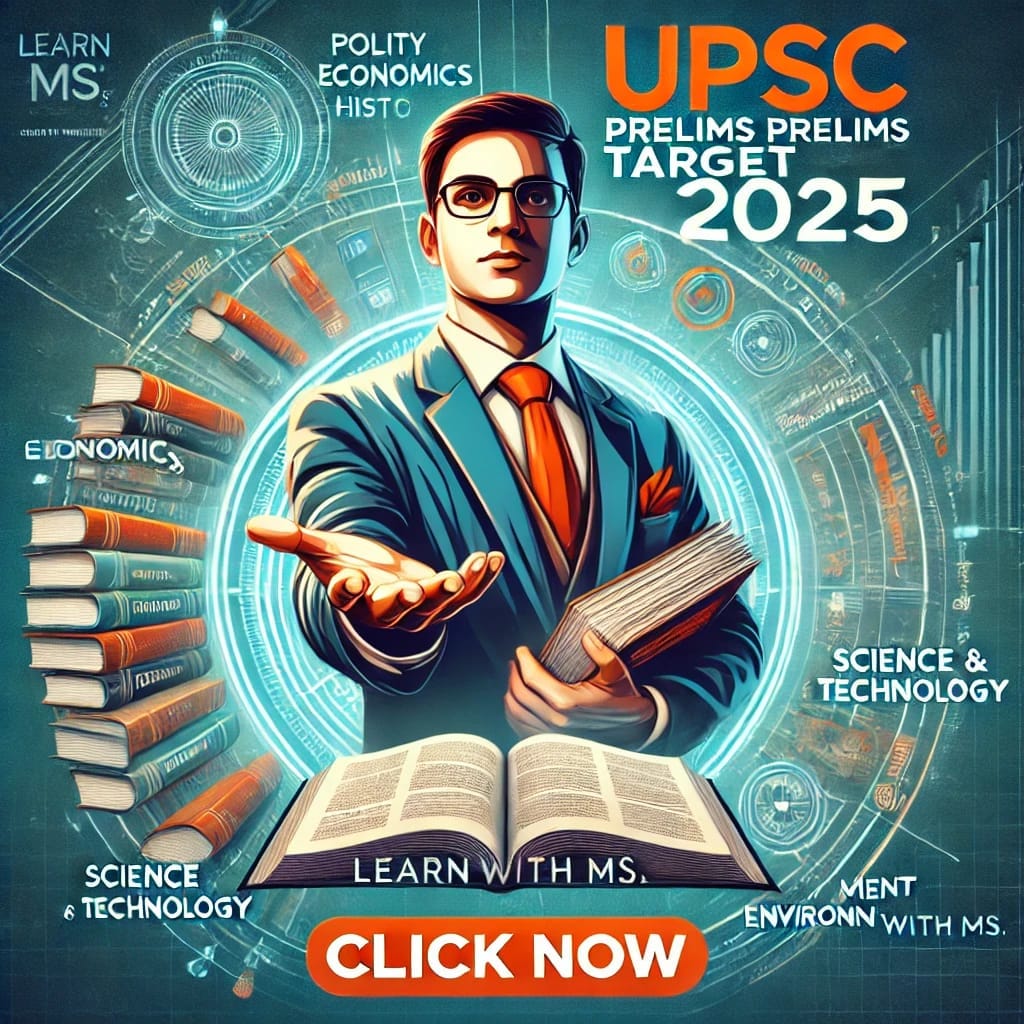
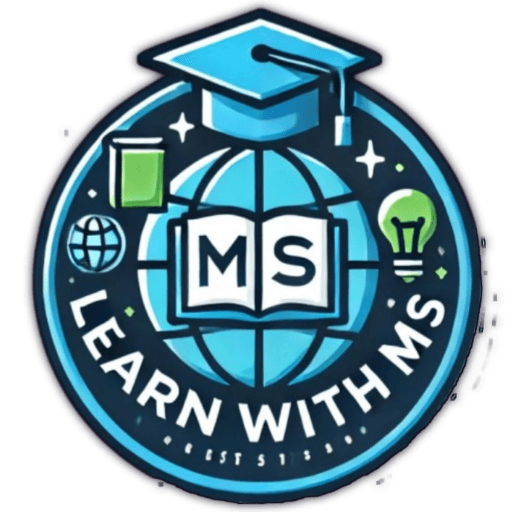
Leave a Reply