DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI FOR UPSC IAS – Prelims And Mains Examination 2025 | 10 March 2025 – UPSC PRELIMS POINTER Fact Based Current Affairs.
DAILY Current Affairs Analysis For UPSC Pre And Mains Examination
Daily Archiveपूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility) और भारत का रुख
पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility) और भारत का रुख
समाचार में क्यों?
• 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत को वर्तमान प्रति व्यक्ति आय ($2,570) के स्तर पर पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Full Capital Account Convertibility) की ओर जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए।
• उनका तर्क है कि पूंजी प्रवाह को पूरी तरह मुक्त करने से आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility) क्या है?
• पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है कि किसी देश की मुद्रा को बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी पूंजी प्रवाह (Capital Flows) के लिए पूरी तरह बदला जा सकता है।
• इससे निवेशक और व्यवसाय आसानी से विदेशी मुद्रा का लेन-देन कर सकते हैं, विदेशी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं और अन्य देशों की मुद्राओं में धन रख सकते हैं।
• जब कोई देश पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देता है, तो वह विदेशी निवेश, कर्ज और अन्य पूंजीगत लेन-देन पर सभी नियंत्रण हटा देता है।
भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता की स्थिति
• भारत ने आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Partial Capital Account Convertibility) को अपनाया है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा प्रवाह पर कुछ नियंत्रण रखता है, विशेष रूप से विदेशी निवेश (FDI, FPI) और बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ECB) के मामलों में।
• चालू खाता (Current Account) पूरी तरह से परिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि व्यापार और सेवा लेन-देन बिना किसी प्रतिबंध के किए जा सकते हैं।
पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संभावित लाभ
• विदेशी निवेश में वृद्धि: निवेशकों के लिए बाजार अधिक आकर्षक बनेगा।
• मुद्रा विनिमय दर का स्थिरीकरण: अधिक विदेशी मुद्रा प्रवाह से भारतीय रुपये को मजबूती मिल सकती है।
• वैश्विक वित्तीय एकीकरण: भारत अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
• निवेशकों के लिए अधिक स्वतंत्रता: भारतीय कंपनियाँ और नागरिक विदेशों में आसानी से निवेश कर सकेंगे।
भारत को पूंजी खाता परिवर्तनीयता में जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए?
• मुद्रा अस्थिरता का खतरा: विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में पूंजी निकासी से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है।
• वित्तीय संकट की संभावना: एशियाई वित्तीय संकट (1997) जैसे उदाहरण बताते हैं कि अनियंत्रित पूंजी प्रवाह आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है।
• बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव: पूर्ण परिवर्तनीयता से बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर अधिक जोखिम बढ़ सकता है।
• नियामक नियंत्रण की कमी: भारत अभी विकसित देशों की तरह मजबूत वित्तीय नियमन प्रणाली नहीं बना पाया है।
भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर अब तक की नीति
| वर्ष | महत्वपूर्ण घटनाएँ |
|---|---|
| 1991 | आर्थिक सुधारों के बाद आंशिक चालू खाता परिवर्तनीयता लागू की गई। |
| 1997 | Tarapore Committee ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए रूपरेखा सुझाई। |
| 2006 | Tarapore Committee (द्वितीय) ने सुझाव दिया कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता को सावधानीपूर्वक लागू किया जाए। |
| 2016 | RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने भी पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रति सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी। |
| 2023 | RBI ने सीमित क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा लेनदेन को सरल बनाया। |
निष्कर्ष:
भारत को पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता अपनाने से पहले अपनी वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाने, विनियमन सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता है।
तब तक, आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता ही आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उपयुक्त विकल्प है।
यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु
GS Paper 3:
• भारतीय अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार।
• RBI की मौद्रिक नीति और वित्तीय विनियमन।
• वैश्विक वित्तीय प्रणाली और भारत।
GS Paper 2:
• आर्थिक सुधार और नीति निर्माण।
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मुद्रा विनिमय नीति।
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) और इसकी चुनौतियाँ – REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) और इसकी चुनौतियाँ
समाचार में क्यों?
• सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया और इसे “निराशाजनक” करार दिया।
• अदालत ने कहा कि RERA का मुख्य उद्देश्य होमबायर्स के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाना था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
RERA क्या है?
• रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित एक नियामक संस्था है।
• इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और होमबायर्स के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।
• प्रत्येक राज्य में RERA प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो रियल एस्टेट परियोजनाओं को पंजीकृत करता है और शिकायतों का निवारण करता है।
RERA के प्रमुख प्रावधान
• रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य (500 वर्ग मीटर या 8 यूनिट से अधिक की परियोजनाओं के लिए)।
• एडवांस पेमेंट की सीमा – बिल्डर केवल 10% तक की राशि अग्रिम रूप से ले सकता है।
• 70% फंड एस्क्रो अकाउंट में – ताकि बिल्डर खरीदारों के धन का दुरुपयोग न कर सके।
• निर्धारित समयसीमा में प्रोजेक्ट पूरा करना अनिवार्य, अन्यथा पेनल्टी।
• शिकायत निवारण प्रणाली – RERA के तहत राज्य स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन।
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के कारण
• RERA में मामलों का धीमा निपटारा, जिससे होमबायर्स को न्याय नहीं मिल रहा।
• राज्यों में RERA के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी – कई राज्य इसे कमजोर कर चुके हैं।
• डेवलपर्स द्वारा नियमों का उल्लंघन जारी – प्रोजेक्ट डिले, पारदर्शिता की कमी।
• होमबायर्स को न्याय दिलाने में असफलता – ग्राहकों को रिफंड और मुआवजा मिलने में कठिनाई।
RERA को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव
• RERA को अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिए जाएं।
• शिकायतों के निपटारे की समयसीमा निर्धारित की जाए।
• होमबायर्स के हितों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं।
• डेवलपर्स द्वारा RERA के आदेशों के पालन को अनिवार्य किया जाए।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
निष्कर्ष:
RERA अधिनियम को होमबायर्स के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं।
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना इस ओर इशारा करती है कि RERA को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।
यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु
GS Paper 2:
• शासन और पारदर्शिता।
• नीतिगत सुधार और नियामक संस्थाएँ।
• उपभोक्ता संरक्षण और न्यायिक सक्रियता।
GS Paper 3:
• बुनियादी ढाँचा (Infrastructure) – रियल एस्टेट क्षेत्र।
• आर्थिक सुधार और कानून।
• अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग सेक्टर।
जनप्रियतावाद (Populism) और सुशासन (Good Governance)
जनप्रियतावाद (Populism) और सुशासन (Good Governance)
समाचार में क्यों?
• भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र से “इमोक्रेसी” (Emocracy) की ओर बढ़ते झुकाव पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता पर बल दिया।
• उन्होंने कहा कि भावनात्मक रूप से संचालित नीतियाँ और विमर्श सुशासन के लिए खतरा बन सकते हैं।
जनप्रियतावाद (Populism) क्या है?
• जनप्रियतावाद (Populism) एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें नेता आम जनता की भावनाओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं, भले ही इससे संस्थागत मूल्यों, कानूनों और दीर्घकालिक नीतियों पर असर पड़े।
• यह अक्सर संवेदनशील मुद्दों, भावनात्मक नारों और तत्काल राहत की रणनीतियों पर आधारित होता है।
• जनप्रियतावादी नेता आमतौर पर जनता को “हम बनाम वे” के आधार पर विभाजित करते हैं, जहाँ वे खुद को जनता का रक्षक और अभिजात्य वर्ग (Elite) का विरोधी बताते हैं।
जनप्रियतावाद और सुशासन के बीच अंतर
| आधार | जनप्रियतावाद (Populism) | सुशासन (Good Governance) |
|---|---|---|
| नीति निर्माण | अल्पकालिक, भावनात्मक निर्णय | दीर्घकालिक, सुविचारित नीति |
| सार्वजनिक भागीदारी | भीड़ के प्रभाव में निर्णय | लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय |
| न्यायपालिका और संस्थाएँ | संस्थानों की अनदेखी, त्वरित समाधान | संस्थाओं का सम्मान, संवैधानिक प्रक्रिया |
| आर्थिक प्रभाव | मुफ्त सुविधाएँ, राजकोषीय बोझ | आर्थिक स्थिरता, टिकाऊ विकास |
| राजनीतिक रणनीति | विभाजनकारी नीतियाँ, जनभावना को भड़काना | समावेशी विकास, समाज की समृद्धि |
जनप्रियतावाद के खतरे
• संस्थानों और कानूनों की अनदेखी: त्वरित लोकप्रियता के लिए सरकारें न्यायपालिका, मीडिया और स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती हैं।
• अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक हानि: मुफ्त योजनाएँ और भावनात्मक निर्णय अल्पकालिक लाभ देते हैं, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकते हैं।
• ध्रुवीकरण (Polarization): जनप्रिय नेता समाज को विभाजित करने वाली नीतियों और नारों का सहारा लेते हैं।
• लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास: भावनात्मक रूप से संचालित शासन जनमत संग्रह (Referendum) और भीड़तंत्र (Mobocracy) की ओर ले जा सकता है।
सुशासन (Good Governance) के तत्व
• जवाबदेही (Accountability): सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
• पारदर्शिता (Transparency): नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ स्पष्ट होनी चाहिए।
• कानून का शासन (Rule of Law): सभी नागरिकों के लिए समान न्याय प्रणाली होनी चाहिए।
• न्यायसंगत विकास (Inclusive Growth): सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
• भागीदारी (Participation): जनता की राय और सहमति से नीतियों का निर्माण।
निष्कर्ष:
लोकतंत्र और सुशासन को संविधान, संस्थानों और दीर्घकालिक नीतियों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल अल्पकालिक भावनात्मक मुद्दों पर।
जनप्रियतावाद भले ही तत्काल लोकप्रियता दिलाए, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए सुशासन ही आवश्यक है।
इसलिए, नीतियों को जनभावनाओं और तर्कसंगत शासन के बीच संतुलन बनाकर बनाया जाना चाहिए।
यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु
GS Paper 2:
• शासन और सुशासन (Governance and Good Governance)।
• लोक प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थाएँ।
• जनप्रियतावाद और उसकी राजनीति पर प्रभाव।
GS Paper 4 (नैतिकता):
• नीति निर्माण और नैतिक दुविधाएँ।
• जवाबदेही और पारदर्शिता।
• लोक प्रशासन में नैतिकता और मूल्यों की भूमिका।
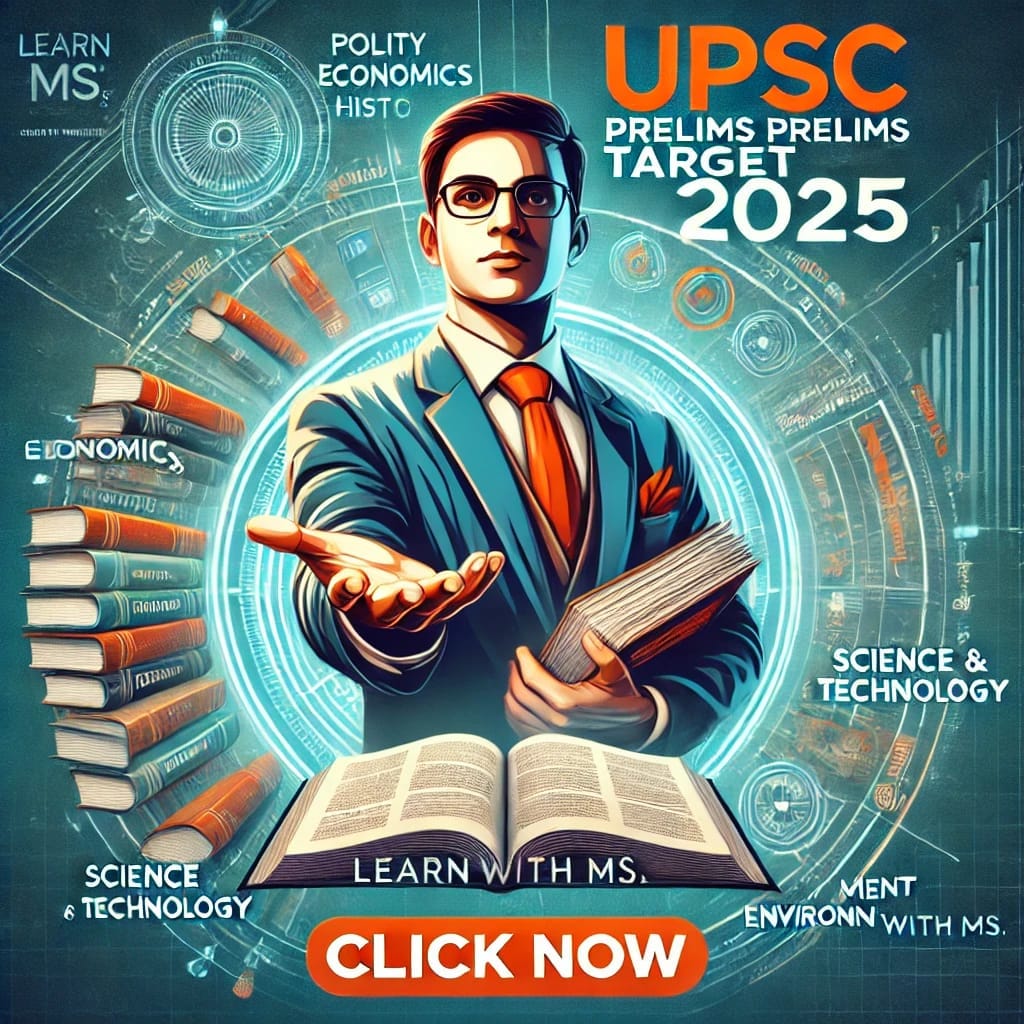
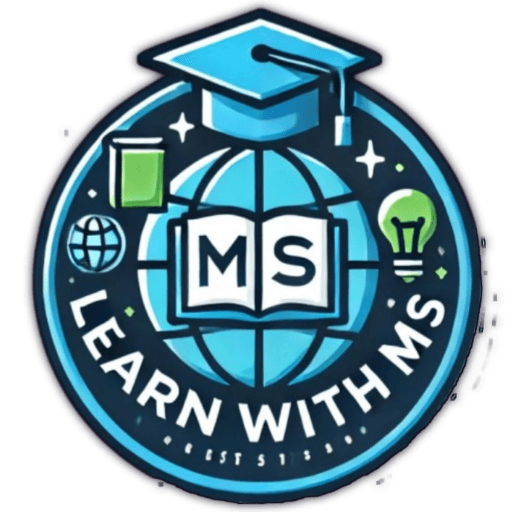
Leave a Reply