संविधान संशोधन अधिनियम | Constitution Ammendment Act (1-105) – UPSC PRELIMS 2025 Based Important and Fact wise
- कुछ महत्वपूर्ण संशोधन
- सभी संवैधानिक संशोधन (1951-2025)
- 1. पहला संशोधन (1951):
- 2. दूसरा संशोधन (1952):
- 3. तीसरा संशोधन (1954):
- 4. चौथा संशोधन (1955):
- 5. पाँचवाँ संशोधन (1955):
- 6. छठा संशोधन (1956):
- 7. सातवाँ संशोधन (1956):
- 8. आठवां संशोधन (1960):
- 9. नौवां संशोधन (1960):
- 10. दसवां संशोधन (1961):
- 11. ग्यारहवां संशोधन (1961):
- 12. बारहवां संशोधन (1962):
- 13. तेरहवां संशोधन (1963):
- 14. चौदहवां संशोधन (1962):
- 15. पंद्रहवां संशोधन (1963):
- 16. सोलहवां संशोधन (1963):
- 17. सत्रहवां संशोधन (1964):
- 18. अठारहवां संशोधन (1966):
- 19. उन्नीसवां संशोधन (1966):
- 20. बीसवां संशोधन (1966):
- 21. इक्कीसवां संशोधन (1967):
- 22. बाईसवां संशोधन (1969):
- 23. तेइसवां संशोधन (1969):
- 24. चौबीसवां संशोधन (1971): (महत्वपूर्ण)
- 25. पच्चीसवां संशोधन (1971): (महत्वपूर्ण)
- 26. छब्बीसवां संशोधन (1971): (महत्वपूर्ण)
- 27. सत्ताईसवां संशोधन (1971):
- 28. अट्ठाईसवां संशोधन (1972):
- 29. उनतीसवां संशोधन (1972):
- 30. तिसवां संशोधन (1973):
- 31. इकत्तीसवां संशोधन (1973):
- 32. बत्तीसवां संशोधन (1973): (महत्वपूर्ण)
- 33. तैंतीसवां संशोधन (1974):
- 34. चौँतीसवां संशोधन (1974):
- 35. पैंतीसवां संशोधन (1974): (महत्वपूर्ण)
- 36. छत्तीसवां संशोधन (1975): (महत्वपूर्ण)
- 37. सैंतीसवां संशोधन (1975):
- 38. अड़तीसवां संशोधन (1975): (महत्वपूर्ण)
- 39. उनतालीसवां संशोधन (1975): (महत्वपूर्ण)
- 40. चालीसवां संशोधन (1976):
- 41. इकतालीसवां संशोधन (1976):
- 42. बयालीसवां संशोधन (1976): (अत्यंत महत्वपूर्ण)
- 43. तेतालिसवां संशोधन (1977):
- 44. चौतालीसवां संशोधन (1978): (महत्वपूर्ण)
- 45. पैंतालीसवां संशोधन (1980):
- 46. छियालीसवां संशोधन (1982):
- 47. सैंतालीसवां संशोधन (1984):
- 48. अठतालीसवां संशोधन (1984):
- 49. उनचासवां संशोधन (1985):
- 50. पचासवां संशोधन (1985):
- 51. इक्यावनवां संशोधन (1987):
- 52. 52th संशोधन (1987):
- 53. तिरेपनवां संशोधन (1989):
- 54. चौवनवां संशोधन (1990):
- 55. पचपनवां संशोधन (1992):
- 56. छप्पनवां संशोधन (1993):
- 56. छप्पनवां संशोधन (1993):
- 57. सत्तावनवां संशोधन (1993):
- 58. अठ्ठावनवां संशोधन (1995):
- 59. उनसठवां संशोधन (1997):
- 60. साठवां संशोधन (1997):
- 61. इकतालीसवां संशोधन (1998):
- 62. बासठवां संशोधन (2002):
- 63. तिरसठवां संशोधन (2002):
- 64. चौसठवां संशोधन (2003):
- 65. पैंसठवां संशोधन (2003):
- 66. छियासठवां संशोधन (2003):
- 67. सत्तासठवां संशोधन (2005):
- 68. अठ्ठासठवां संशोधन (2005):
- 69. उनसठवां संशोधन (2006):
- 70. सत्तरवां संशोधन (2006):
- 71. इकतिहत्तरवां संशोधन (2008):
- 72. बहत्तरवां संशोधन (2008):
- 73. तिहत्तरवां संशोधन (1992):
- 74. चौहत्तरवां संशोधन (1992):
- 75. पचहत्तरवां संशोधन (1994):
- 76. छियत्तरवां संशोधन (1994):
- 77. सत्ताहत्तरवां संशोधन (1995):
- 78. अठत्तरवां संशोधन (1995):
- 79. उनासीवां संशोधन (2000):
- 80. अस्सीवां संशोधन (2000):
- 81. इक्यासीवां संशोधन (2000):
- 82. बयासीवां संशोधन (2002):
- 83. तिरासीवां संशोधन (2002):
- 84. चौरासीवां संशोधन (2002):
- 85. पचासीवां संशोधन (2002):
- 86. छियासीवां संशोधन (2002):
- 87. सत्तासीवां संशोधन (2003):
- 88. अठासीवां संशोधन (2004):
- 89. नवासीवां संशोधन (2005):
- 90. नब्बेवां संशोधन (2005):
- 91. इक्यासीवां संशोधन (2003): 91th Constitution Amendment Act
- 92. बानवेवां संशोधन (2003): 92th Constitution Amendment Act
- 93. तिरानवेवां संशोधन (2005): 93th Constitution Amendment Act
- 94. चौरानवेवां संशोधन (2005): 94th Constitution Amendment Act
- 95. पचानवेवां संशोधन (2006): 95th Constitution Amendment Act
- 96. छियानवेवां संशोधन (2007): 96th Constitution Amendment Act
- 97. सत्तानवेवां संशोधन (2007): 97th Constitution Amendment Act
- 98. अठानवेवां संशोधन (2007): 98th Constitution Amendment Act
- 99. निन्यानवेवां संशोधन (2008): 99th Constitution Amendment Act
- 100. शताबदी संशोधन (2008): 100th Constitution Amendment Act
- 101. एकसौ एकवां संशोधन (2016): 101th Constitution Amendment Act
- 102. एकसौ दूसरी संशोधन (2018): 102 Constitution Amendment Act
- 103. एकसौ तीसरी संशोधन (2019): 103rd Constitution Amendment Act
- 104. एकसौ चौथा संशोधन (2019): 104th Constitution Amendment Act
- 105. एकसौ पांचवां संशोधन (2020): 105th Constitution Amendment Act
कुछ महत्वपूर्ण संशोधन
भारतीय संविधान के सभी संशोधनों को विस्तार से समझने के लिए, हम उन्हें कालक्रम के अनुसार और उनके महत्व के आधार पर देखेंगे। यहाँ मैं प्रमुख संशोधनों के साथ उनके ऐतिहासिक और संवैधानिक संदर्भ को और विस्तार में बताऊंगा।
पहला संशोधन (1951):
पृष्ठभूमि:
1950 में संविधान लागू होने के बाद यह महसूस हुआ कि कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है, विशेष रूप से भूमि सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों में।
मुख्य प्रावधान:
- नौवीं अनुसूची की स्थापना:
- भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयीय समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
- उद्देश्य था कि न्यायालय इन कानूनों को मौलिक अधिकारों के खिलाफ न ठहराए।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध:
- अनुच्छेद 19(1)(a) में “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” पर ‘सार्वजनिक व्यवस्था’, ‘राज्य की सुरक्षा’ और ‘शिष्टाचार’ जैसे प्रतिबंध जोड़े गए।
- सामाजिक और आर्थिक न्याय:
- राज्य को पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई।
सातवां संशोधन (1956):
पृष्ठभूमि:
भारत के राज्यों का गठन भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर हुआ था। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई थी।
मुख्य प्रावधान:
- राज्यों का पुनर्गठन:
- भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र।
- A, B, C, D श्रेणियों को समाप्त करके केवल “राज्य” और “केंद्रशासित प्रदेश” बनाया गया।
- राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन:
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया गया।
42वां संशोधन (1976):
पृष्ठभूमि:
यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया। इसे “मिनी संविधान” भी कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक और गहरे बदलाव किए गए।
मुख्य प्रावधान:
- संविधान की प्रस्तावना में बदलाव:
- “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए।
- “एकता और अखंडता” शब्द जोड़े गए।
- मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना:
- अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
- न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती:
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित किया गया।
- राज्य नीति के निर्देशक तत्व:
- DPSP को लागू करने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका:
- कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया और न्यायपालिका को कमजोर किया गया।
44वां संशोधन (1978):
पृष्ठभूमि:
42वें संशोधन की आलोचना के बाद जनता पार्टी सरकार ने इसे संतुलित करने के लिए 44वां संशोधन लाया।
मुख्य प्रावधान:
- संपत्ति का अधिकार:
- अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बनाया गया।
- आपातकाल के प्रावधान:
- राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए “आंतरिक अशांति” को बदलकर “सशस्त्र विद्रोह” कर दिया गया।
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा:
- मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के नियम सख्त किए गए।
73वां और 74वां संशोधन (1992):
पृष्ठभूमि:
पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए यह संशोधन लाया गया।
मुख्य प्रावधान:
- पंचायती राज व्यवस्था (73वां):
- अनुच्छेद 243 से 243O और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- ग्राम सभा, पंचायतों के चुनाव और उनके कार्यों का प्रावधान।
- शहरी स्थानीय निकाय (74वां):
- अनुच्छेद 243P से 243ZG और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- नगर पालिकाओं की संरचना और शक्तियों को परिभाषित किया गया।
86वां संशोधन (2002):
पृष्ठभूमि:
शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 21A का प्रावधान:
- 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
- मौलिक कर्तव्य:
- माता-पिता और अभिभावकों के लिए बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य।
101वां संशोधन (2016):
पृष्ठभूमि:
भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए यह संशोधन लाया गया।
मुख्य प्रावधान:
- GST लागू करना:
- वस्तु और सेवा कर (GST) के लिए एकल कर प्रणाली।
- केंद्र और राज्यों के अधिकारों को परिभाषित करना।
- अनुच्छेद 246A, 269A और 279A:
- GST काउंसिल की स्थापना।
105वां संशोधन (2021):
पृष्ठभूमि:
ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की पहचान का अधिकार राज्य सरकारों को वापस देने के लिए यह संशोधन लाया गया।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 342A में संशोधन:
- राज्य सरकारों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया:
भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए तीन प्रक्रियाएँ होती हैं:
- साधारण बहुमत से:
जैसे राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े संशोधन। - विशेष बहुमत से:
जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन। - विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से:
जैसे संघीय ढांचे से जुड़े संशोधन।
निष्कर्ष:
भारतीय संविधान में किए गए संशोधन समय के साथ बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। ये संशोधन भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को मजबूत करने में सहायक रहे हैं।
सभी संवैधानिक संशोधन (1951-2025)
भारतीय संविधान के 105 संशोधनों को एक-एक करके विस्तार से चर्चा करना काफी व्यापक कार्य है। हर संशोधन को एक संदर्भ, उद्देश्य, और प्रभाव के आधार पर देखना होगा। मैं यहाँ सभी संशोधनों को क्रमबद्ध तरीके से विस्तृत चर्चा में प्रस्तुत करता हूँ।
1. पहला संशोधन (1951):
पृष्ठभूमि:
संविधान लागू होने के तुरंत बाद, भूमि सुधार कानूनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर चुनौतियाँ सामने आईं। न्यायपालिका ने कई कानूनों को असंवैधानिक ठहराया, जिससे सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा।
मुख्य प्रावधान:
- नौवीं अनुसूची का निर्माण:
- भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में डाला गया, ताकि वे न्यायालयीय समीक्षा से बच सकें।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबंध:
- अनुच्छेद 19(1)(a) में ‘सार्वजनिक व्यवस्था’, ‘राज्य की सुरक्षा’ और ‘शिष्टाचार’ जैसे प्रतिबंध जोड़े गए।
- सामाजिक और आर्थिक न्याय:
- राज्य को पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई।
प्रभाव:
- भूमि सुधार कानूनों को संरक्षित किया गया।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रित किया गया।
2. दूसरा संशोधन (1952):
पृष्ठभूमि:
लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के पुनः निर्धारण की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि इसे जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जा सके।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 81 में संशोधन:
- लोकसभा में सीटों की संख्या को 500 तक सीमित किया गया।
- प्रति सदस्य की जनसंख्या का अनुपात:
- प्रति लोकसभा सदस्य की औसत जनसंख्या का निर्धारण किया गया।
प्रभाव:
- जनसंख्या के आधार पर सीटों का वितरण सुनिश्चित हुआ।
- प्रतिनिधित्व अधिक समान और संतुलित बना।
3. तीसरा संशोधन (1954):
पृष्ठभूमि:
राज्यों के पुनर्गठन और केंद्र को अधिक प्रशासनिक अधिकार देने के लिए संशोधन की आवश्यकता हुई।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 3 और 4 में संशोधन:
- संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया।
- नए राज्यों का गठन:
- भाषा और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर नए राज्यों के निर्माण का प्रावधान।
प्रभाव:
- राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया।
- केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन मजबूत हुआ।
4. चौथा संशोधन (1955):
पृष्ठभूमि:
राज्य को संपत्ति के अधिकार और अन्य मुद्दों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए यह संशोधन लाया गया।
मुख्य प्रावधान:
- संपत्ति के अधिकार:
- राज्य को संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार दिया गया।
- नौवीं अनुसूची में और अधिक कानून जोड़ना:
- भूमि सुधार कानूनों और अन्य समाजवादी नीतियों को सुरक्षित किया गया।
प्रभाव:
- भूमि सुधार प्रक्रिया को तेज किया गया।
- संपत्ति के अधिकार को राज्य के अधीन किया गया।
5. पाँचवाँ संशोधन (1955):
पृष्ठभूमि:
राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में संविधान की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता थी।
मुख्य प्रावधान:
- राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की सहमति:
- राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य की गई।
प्रभाव:
- राज्यों की सीमाओं में बदलाव अधिक संगठित और वैधानिक बना।
6. छठा संशोधन (1956):
पृष्ठभूमि:
राज्यों को करों और वित्तीय अधिकारों के बेहतर वितरण के लिए यह संशोधन लाया गया।
मुख्य प्रावधान:
- राज्यों के वित्तीय अधिकार:
- केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण में संशोधन।
- राज्यों को स्थानीय कर लगाने का अधिकार:
- राज्यों को कुछ करों पर विशेष अधिकार दिए गए।
प्रभाव:
- वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला।
- केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण अधिक स्पष्ट हुआ।
7. सातवाँ संशोधन (1956):
पृष्ठभूमि:
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन लाया गया।
मुख्य प्रावधान:
- राज्यों का पुनर्गठन:
- भाषाई आधार पर राज्यों का गठन।
- चार श्रेणियों (A, B, C, D) के राज्यों को समाप्त किया गया।
- केंद्रशासित प्रदेश:
- केंद्रशासित प्रदेशों की अवधारणा को लागू किया गया।
प्रभाव:
- भारत में राज्यों का नया स्वरूप तैयार हुआ।
- भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान मिला।
8. आठवां संशोधन (1960):
पृष्ठभूमि:
भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के बाद बांग्लादेश सीमा (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) के क्षेत्रों में बदलाव को वैध बनाने की जरूरत थी।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 3 में संशोधन:
- भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के अनुसार, कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का भारत से पाकिस्तान में स्थानांतरण।
प्रभाव:
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों का समाधान किया गया।
9. नौवां संशोधन (1960):
पृष्ठभूमि:
भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश सीमा के तहत हुए समझौते को संवैधानिक रूप से लागू करने के लिए।
मुख्य प्रावधान:
- भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण:
- भारत से पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र सौंपे गए।
प्रभाव:
- अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बढ़ावा मिला।
10. दसवां संशोधन (1961):
पृष्ठभूमि:
गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 240 में संशोधन:
- गोवा, दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया।
प्रभाव:
- भारतीय संघ का क्षेत्रीय विस्तार हुआ।
11. ग्यारहवां संशोधन (1961):
पृष्ठभूमि:
उपराष्ट्रपति के चुनाव और उनके कार्यों को स्पष्ट करने के लिए।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन:
- उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन।
प्रभाव:
- कार्यकारी शक्ति का संतुलन सुनिश्चित हुआ।
12. बारहवां संशोधन (1962):
पृष्ठभूमि:
सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 371 में संशोधन:
- सिक्किम को “भारत के सहायक राज्य” का दर्जा दिया गया।
प्रभाव:
- सिक्किम के भारत में एकीकरण का पहला कदम।
13. तेरहवां संशोधन (1963):
पृष्ठभूमि:
नागालैंड को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 371A का प्रावधान:
- नागालैंड को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई।
प्रभाव:
- नागालैंड की सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को मान्यता मिली।
14. चौदहवां संशोधन (1962):
पृष्ठभूमि:
पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 239 और 240 में संशोधन:
- पुडुचेरी को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
प्रभाव:
- पुडुचेरी का भारत में पूर्ण एकीकरण हुआ।
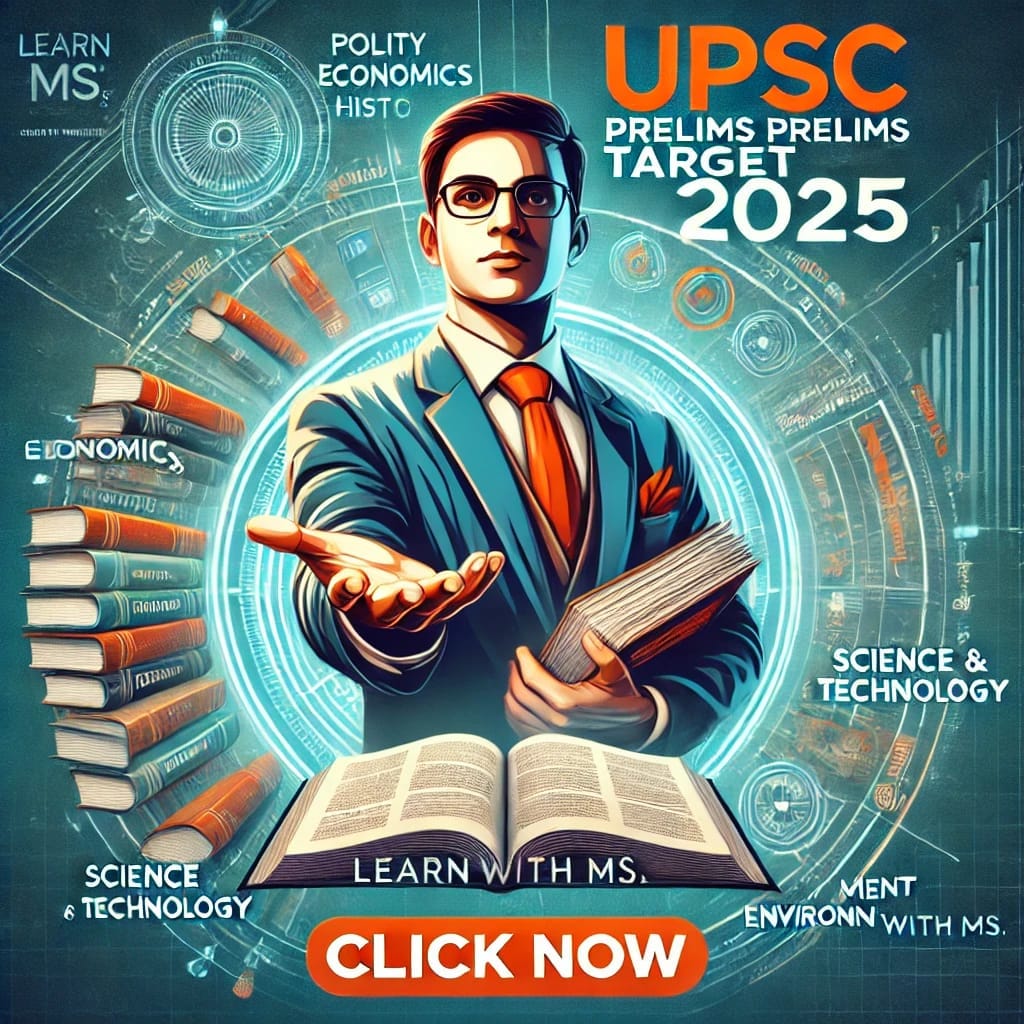
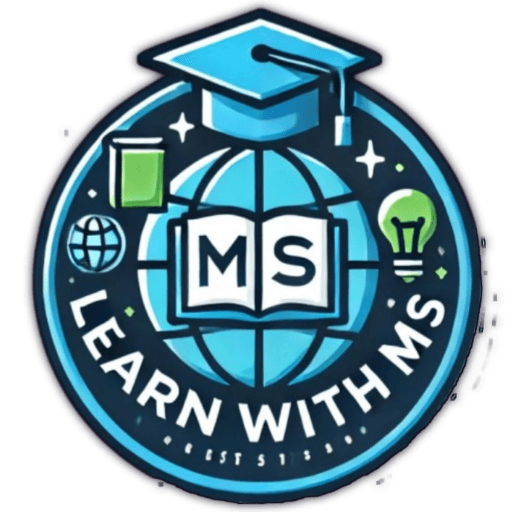
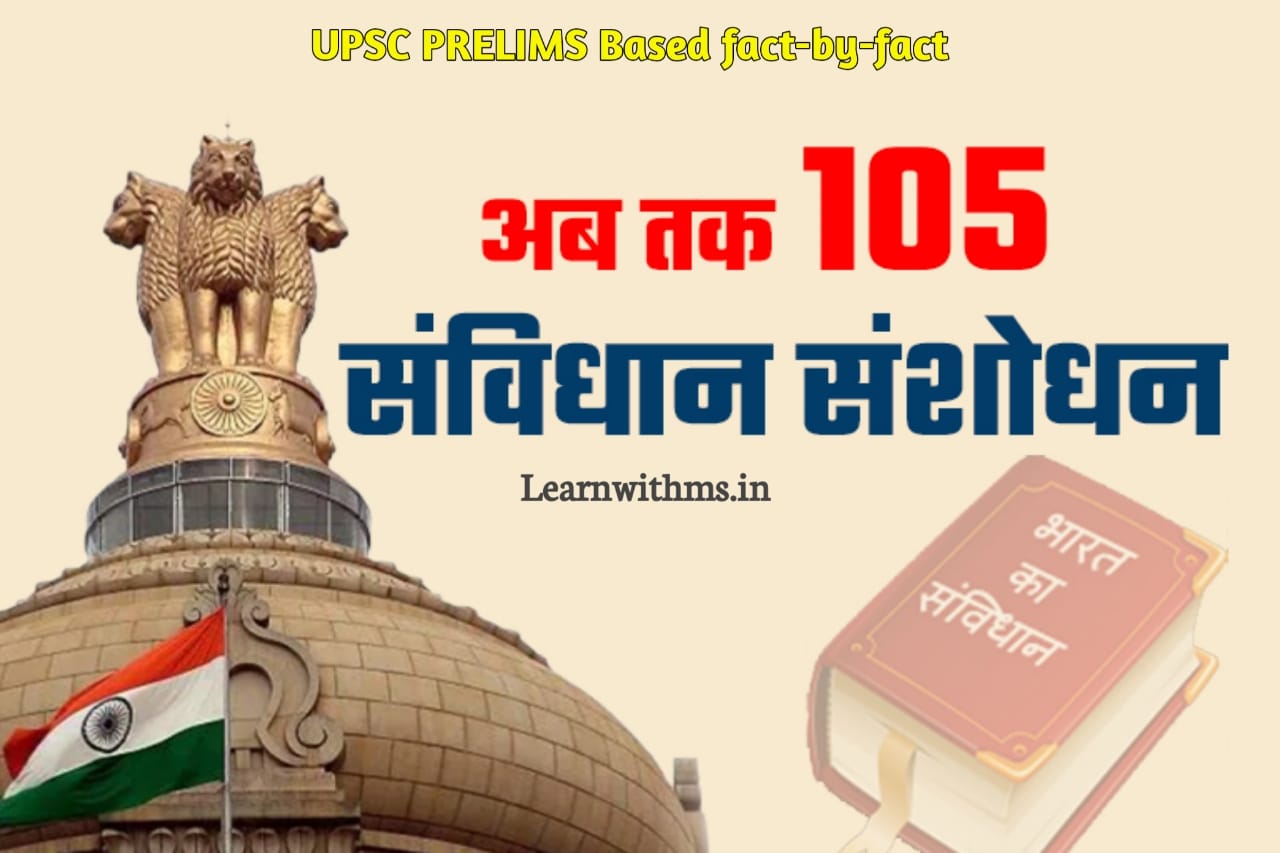
Leave a Reply