- भारतीय संविधान की मूल संरचना एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
- परिचय:
- 1. चंपकम दोराईराजन बनाम राज्य (1951)
- 2. शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
- 3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- 4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
- 5. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
- 6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
- 7. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
- 8. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
भारतीय संविधान की मूल संरचना एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
परिचय:
भारतीय संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) वह सिद्धांत है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा या बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती।
मूल संरचना की अवधारणा कैसे आई?
🔹 “मूल संरचना सिद्धांत” को भारतीय संविधान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था।
🔹 इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
संविधान की मूल संरचना के प्रमुख तत्व:
सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में भारतीय संविधान की मूल संरचना के कुछ तत्व निर्धारित किए हैं:
1️⃣ संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)
2️⃣ संप्रभुता, लोकतंत्र और गणराज्यात्मक स्वरूप (Sovereignty, Democracy, and Republican Nature)
3️⃣ न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary)
4️⃣ संघीय स्वरूप (Federal Character of the Constitution)
5️⃣ मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
6️⃣ संविधान के निर्देशित नीति तत्व (DPSP) का महत्व
7️⃣ लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया
8️⃣ कानून का शासन (Rule of Law)
9️⃣ भारत की एकता और अखंडता (Unity and Integrity of India)
🔟 न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)
🔹 संविधान में संतुलन और शक्ति पृथक्करण (Balance & Separation of Powers)
महत्व:
✅ यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक सुरक्षा की ढाल है।
✅ यह संसद को मनमाने संशोधन करने से रोकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है।
✅ संविधान की स्थिरता और लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय (Judgments of Supreme Court)
1. चंपकम दोराईराजन बनाम राज्य (1951)
🔹 यह निर्णय भारतीय संविधान में आरक्षण नीति से संबंधित पहला ऐतिहासिक फैसला था।
🔹 इसमें न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) निर्देशित नीति तत्वों (DPSP) से ऊपर होते हैं।
2. शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
🔹 यह पहला मामला था जिसमें न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संशोधन अधिकार को बरकरार रखा।
🔹 इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
🔹 इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
🔹 इस फैसले ने अनुच्छेद 368 की व्याख्या को सीमित कर दिया।
4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
🔹 “मूल संरचना सिद्धांत” की स्थापना इसी निर्णय में की गई।
🔹 इस फैसले में कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
🔹 इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की आधारशिला रखी।
5. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
🔹 इस मामले में न्यायालय ने निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया।
🔹 आपातकाल (Emergency) के दौरान यह फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ।
6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
🔹 इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि संविधान का संतुलन (Balance) बनाए रखना आवश्यक है।
🔹 संसद मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) और निर्देशित नीति तत्वों (DPSP) में संतुलन बनाए रखे।
7. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
🔹 इस फैसले में कहा गया कि संविधान की “संघीय संरचना” भी मूल संरचना का हिस्सा है।
🔹 राज्यों में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने की सीमा निर्धारित की गई।
8. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
🔹 इस फैसले में न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक कर दिया।
🔹 न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया।
नीचे दी गई तालिका में भारतीय संविधान की मूल संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को प्रस्तुत किया गया है:
| क्र. सं. | मुकदमे का नाम (वर्ष) | मूलभूत ढांचे के तत्व (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित) |
|---|---|---|
| 1. | केशवानंद भारती मामला (1973) | संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति संतुलन, गणराज्य और लोकतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, संघीय चरित्र, संप्रभुता और एकता, स्वतंत्रता और गरिमा, कल्याणकारी राज्य, संसदीय प्रणाली |
| 2. | इंदिरा नेहरू गांधी मामला (1975) | लोकतंत्र, चुनावों की स्वतंत्रता |
| 3. | मिन्नर्वा मिल्स मामला (1980) | न्यायिक समीक्षा, मूल संरचना की संकल्पना |
| 4. | संदीप कोलेज लाइमिटेड मामला (1980) | विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन |
| 5. | एस.आर. बोम्मई मामला (1994) | धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, न्यायिक समीक्षा |
| 6. | पी. समथियामूर्ति मामला (1987) | कानून का शासन |
| 7. | दिल्ली अडमिनिस्ट्रेशन सिविल एसोसिएशन मामला (1991) | अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत न्यायिक शक्ति |
| 8. | इंद्रा साहनी मामला (1992) | आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय |
| 9. | किहोटो होलोहोन मामला (1993) | स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव |
| 10. | कुशुम लता मामला (2006) | स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव |
| 11. | राम जेठमलानी मामला (2011) | न्यायिक समीक्षा |
| 12. | नमित शर्मा मामला (2013) | व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा |
| 13. | मद्रास बार एसोसिएशन मामला (2014) | अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां |
निष्कर्ष:
भारतीय संविधान की मूल संरचना देश के लोकतांत्रिक, गणराज्यात्मक और संप्रभु स्वरूप को बनाए रखने में सहायक है। यह न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि संसद संविधान में ऐसे कोई संशोधन न करे, जो उसकी मूल भावना को प्रभावित करे। 🚩📜
“मूल संरचना सिद्धांत” भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
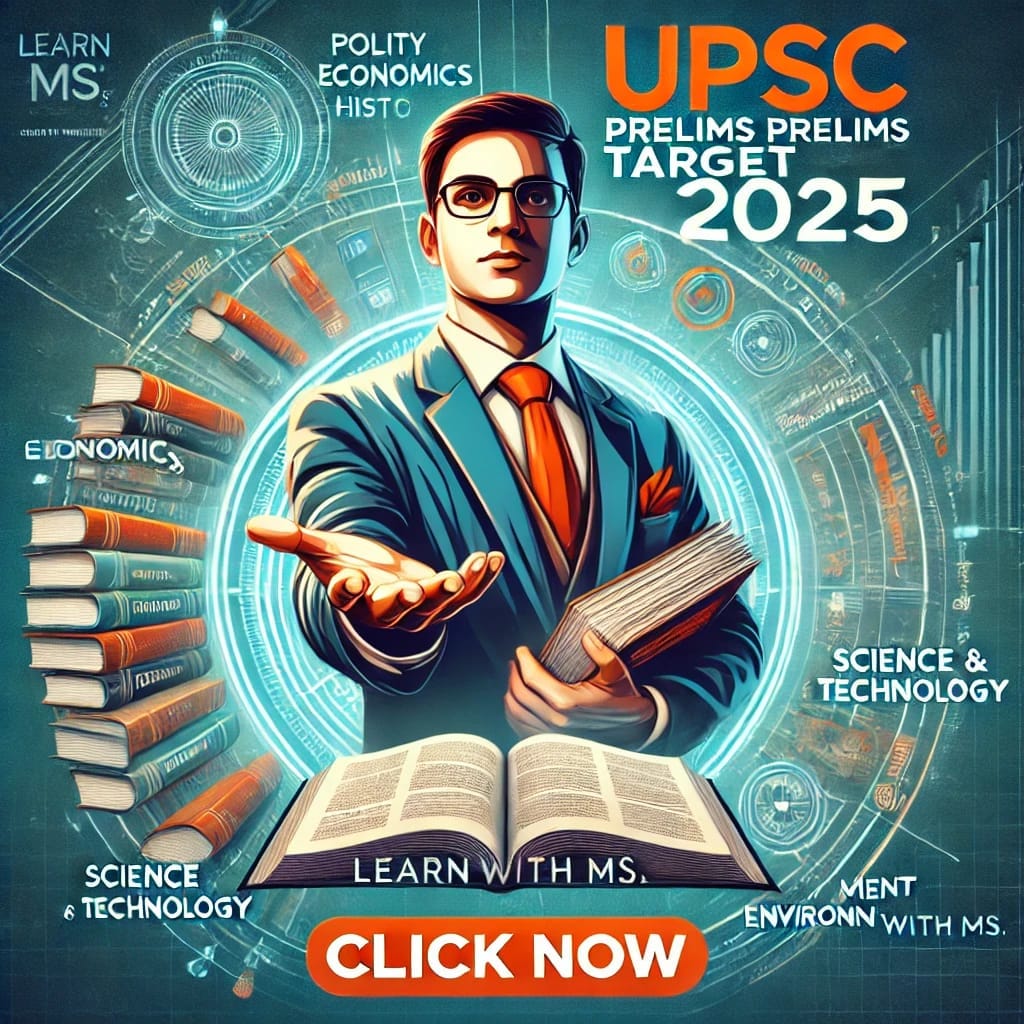
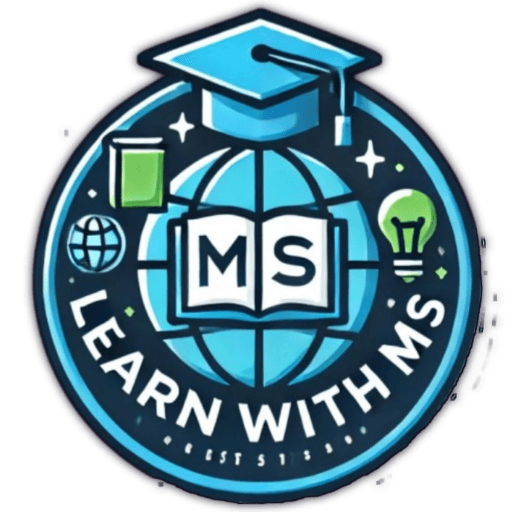
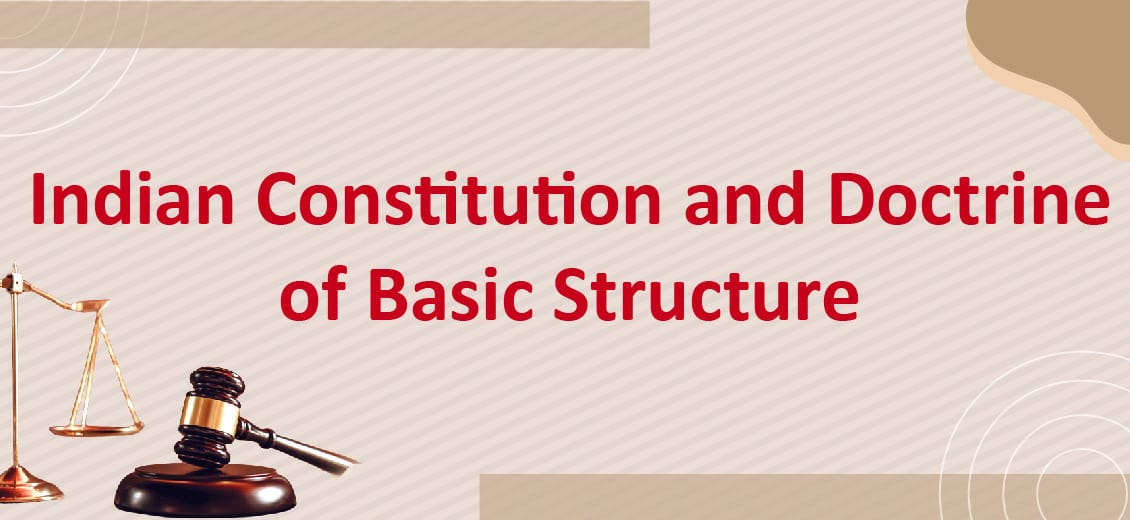
Leave a Reply