समाचार में क्यों?
• उत्तराखंड के चमोली जिले में सीमा सड़क संगठन (BRO) के एक परियोजना स्थल पर शुक्रवार को हिमस्खलन (Avalanche) आया।
• रविवार तक चार और शव बरामद किए गए, जिससे इस आपदा में मरने वालों की संख्या 8 हो गई।
• यह घटना उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते हिमस्खलन के खतरे को उजागर करती है।
हिमस्खलन (Avalanche) क्या है?
• परिभाषा: हिमस्खलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बर्फ, बर्फ के टुकड़े, चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे की ओर खिसकते हैं।
• यह मुख्यतः पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में होता है।
• अत्यधिक हिमस्खलन भारी विनाश, जान-माल की हानि और बुनियादी ढांचे के नुकसान का कारण बन सकता है।
हिमस्खलन के कारण
- प्राकृतिक कारण:
• अत्यधिक बर्फबारी और तापमान में परिवर्तन।
• भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से कंपन।
• तेज हवा और हिमपात से अस्थिरता। - मानवजनित कारण:
• निर्माण कार्य और सड़कों की खुदाई।
• पर्यटन और मानव गतिविधियों में वृद्धि।
• वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन।
उत्तराखंड में हिमस्खलन और जोखिम
• उत्तराखंड का चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला हिमस्खलन के लिए संवेदनशील हैं।
• फरवरी 2021 में चमोली में ग्लेशियर टूटने से भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे।
• BRO और अन्य निर्माण परियोजनाएँ जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
रोकथाम और बचाव उपाय
• हिमस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली (Avalanche Forecasting System) का विकास।
• ग्लेशियरों और बर्फीले क्षेत्रों की निरंतर निगरानी।
• स्थानीय समुदायों और बचाव दल को प्रशिक्षण।
• पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास रणनीतियाँ।
मुख्य निष्कर्ष
हिमस्खलन (Avalanche) क्या है?
- हिमस्खलन बर्फ, बर्फीले टुकड़ों और मलबे का अचानक और तीव्र गति से पहाड़ी ढलान पर गिरना है।
- यह प्राकृतिक या मानव-जनित कारणों से उत्पन्न हो सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी विनाश ला सकता है।
हिमस्खलन के प्रकार
- लूज़ स्नो हिमस्खलन – एक बिंदु से शुरू होकर नीचे आते हुए अपना आकार बढ़ाता है।
- स्लैब हिमस्खलन – बर्फ की एक बड़ी परत टूटकर गिरती है, यह सबसे खतरनाक प्रकार है।
- पाउडर स्नो हिमस्खलन – ढीली बर्फ और हवा का मिश्रण, जो तेज गति से चलता है।
- वेट स्नो हिमस्खलन – पिघलती बर्फ के कारण होता है, गति कम लेकिन अत्यधिक विनाशकारी होता है।
हिमस्खलन के कारण
✅ प्राकृतिक कारण
- भारी बर्फबारी – बर्फ की परतों का भार बढ़ता है।
- तापमान में बदलाव – बर्फ की संरचना कमजोर होती है।
- बारिश या बर्फ का पिघलना – बर्फ की परतों के जुड़ाव को कमजोर करता है।
- भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट – बर्फ की परतों में हलचल पैदा करता है।
✅ मानव-जनित कारण
- वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन – पहाड़ी ढलानों को अस्थिर करता है।
- निर्माण, खनन, विस्फोटों से उत्पन्न कंपन – हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकता है।
- एडवेंचर पर्यटन और स्कीइंग – हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में बर्फीली सतह को अस्थिर करता है।
हिमस्खलन के प्रभाव
- जान-माल की हानि – हिमालयी क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश)।
- आर्थिक क्षति – सड़कों, बिजली लाइनों और संचार नेटवर्क को नुकसान।
- पर्यावरणीय गिरावट – वनों की कटाई, भूस्खलन, और प्राकृतिक आवास का विनाश।
- सैन्य बलों पर प्रभाव – सियाचिन ग्लेशियर और ऊँचाई वाले सैन्य ठिकानों में सैनिकों की हानि।
रोकथाम और तैयारी
✅ हिमस्खलन की भविष्यवाणी और निगरानी
- DRDO का स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट (SASE) वास्तविक समय पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का उपयोग अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए किया जाता है।
✅ संरचनात्मक उपाय
- हिमस्खलन अवरोधक, बर्फ शेड, और नियंत्रित विस्फोट से हिमस्खलन रोका जाता है।
- वनारोपण और ढलान स्थिरीकरण से जोखिम कम किया जाता है।
✅ आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और स्थानीय एजेंसियाँ बचाव कार्यों का संचालन करती हैं।
- सैन्य बलों और स्थानीय लोगों को हिमस्खलन से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु
GS Paper 3:
• आपदा प्रबंधन और हिमस्खलन से निपटने की रणनीति।
• जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव।
• सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यावरणीय प्रभाव।
GS Paper 1:
• हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ और उनसे उत्पन्न चुनौतियाँ।
निष्कर्ष:
उत्तराखंड और अन्य हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की बढ़ती घटनाएँ जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास का संकेत देती हैं। सरकार को बेहतर आपदा प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और सतत विकास नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।
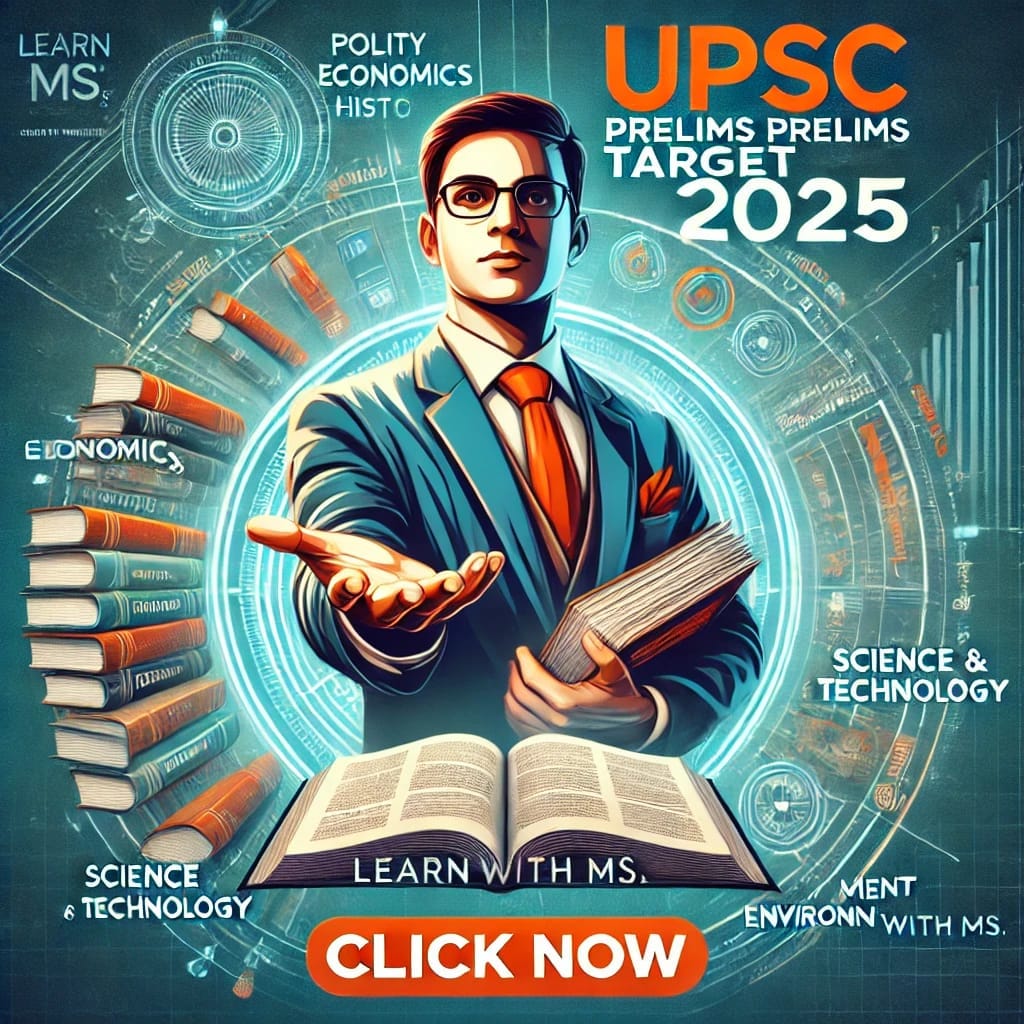
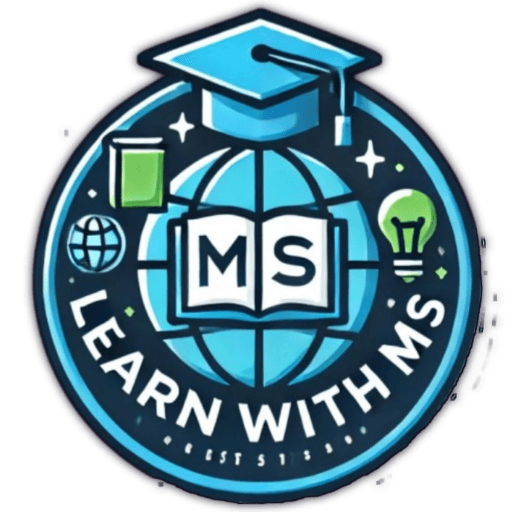
Leave a Reply