- चर्चा में क्यों?
- 1. सूचना आयोग और सूचना आयुक्तों का कार्य
- 2. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया
- 3. नियुक्ति में देरी के कारण
- 4. इसके परिणाम और प्रभाव
- 5. समाधान और सुधार के उपाय
- 6. उदाहरण
- निष्कर्ष
- 1. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का परिचय
- 2. सूचना आयोग और सूचना आयुक्तों की भूमिका
- 3. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति
- 4. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी और RTI अधिनियम का प्रभाव
- 5. RTI के तहत शिकायतों और अपीलों का निपटान
- 6. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के कारण
- 7. कानूनी और न्यायिक हस्तक्षेप
- 8. उपसंहार
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम, 2005) के तहत सूचना आयुक्तों (IC) की नियुक्ति में केंद्र तथा राज्यों द्वारा की जा रही लगातार देरी की निंदा की है।
- सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी से नागरिकों की सूचना के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता सीमित होने के साथ मामले लंबित रहते हैं।
सूचना आयोग – कार्य, नियुक्त, कारण
1. सूचना आयोग और सूचना आयुक्तों का कार्य
सूचना आयोग, जिसे केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC) के रूप में विभाजित किया गया है, भारत में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिल सके और यदि किसी सरकारी संस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो उसकी अपील और शिकायतों का समाधान किया जा सके। सूचना आयुक्त आयोग के मुख्य कार्यकारी होते हैं और उनकी नियुक्ति आयोग की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।
2. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
- उम्मीदवारों की चयन समिति: सूचना आयुक्तों का चयन केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्षी नेता की समिति द्वारा किया जाता है।
- योग्यता: यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवार की योग्यता और अनुभव सूचना आयोग में कार्य करने के लिए उपयुक्त हो।
- प्रकाशन और साक्षात्कार: नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों के चयन के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं और साक्षात्कार लिया जाता है।
3. नियुक्ति में देरी के कारण
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के पीछे कई प्रमुख कारण हो सकते हैं:
a) राजनीतिक कारण
- अक्सर नियुक्तियों में राजनीतिक कारणों का हस्तक्षेप होता है। सरकार अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को नियुक्त करने का प्रयास करती है, जो कभी-कभी समय लेता है।
- विपक्षी दल और अन्य संगठनों द्वारा नियुक्तियों में हस्तक्षेप की शिकायतें भी उठाई जाती हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है।
b) चुनाव प्रक्रिया की जटिलताएँ
- उम्मीदवारों का चयन और साक्षात्कार की प्रक्रिया जटिल और समय-consuming होती है। कई बार यह चयन पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता, जिससे इसमें देरी होती है।
c) अयोग्य उम्मीदवारों का चयन
- कभी-कभी चयन समिति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाता, जिसके कारण पुनः चयन की प्रक्रिया शुरू होनी पड़ती है।
d) संसदीय और कानूनी विलंब
- कई बार संसद की कार्यवाही में देरी होती है, जिससे चयन प्रक्रिया की गति धीमी हो जाती है। कानूनों में बदलाव या संशोधन की आवश्यकता भी देरी का कारण बन सकती है।
4. इसके परिणाम और प्रभाव
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के अनेक गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो सूचना के अधिकार पर सीधा प्रभाव डालते हैं:
a) सूचना के अधिकार का हनन
- सूचना आयोग के बिना नागरिकों की शिकायतों का उचित समाधान नहीं हो पाता। बिना सूचना आयुक्त के कार्यवाही में रुकावट आती है, और नागरिकों का अधिकार प्रभावित होता है।
b) प्रशासनिक निष्क्रियता
- यदि आयुक्तों की नियुक्ति में देरी होती है, तो सरकारी विभागों और संस्थाओं के खिलाफ नागरिकों द्वारा की गई अपीलों का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता।
c) न्यायिक हस्तक्षेप
- कई बार न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे यह मुद्दा और जटिल हो जाता है। कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन यह सरकार के कार्यों को प्रभावित करता है।
d) सार्वजनिक विश्वास में कमी
- लगातार देरी के कारण जनता का सरकारी संस्थाओं पर विश्वास कम हो सकता है, विशेष रूप से सूचना के अधिकार के प्रति।
5. समाधान और सुधार के उपाय
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, ताकि इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके:
a) पारदर्शिता में वृद्धि
- चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्रता लानी चाहिए, ताकि राजनीतिक दबाव कम हो सके और उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जा सके।
b) समय सीमा तय करना
- नियुक्ति के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, ताकि इसमें देरी को नियंत्रित किया जा सके।
c) स्वतंत्र संस्थाओं का गठन
- एक स्वतंत्र संस्था, जो राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, नियुक्तियों की निगरानी और समीक्षा कर सकती है। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकती है।
d) न्यायिक हस्तक्षेप से बचाव
- यदि नियुक्ति में देरी हो रही है, तो न्यायपालिका को प्राथमिक तौर पर हस्तक्षेप करने के बजाय प्रभावी माध्यमों के द्वारा सरकार पर दबाव डालने के उपायों का पालन किया जा सकता है।
6. उदाहरण
भारत में कई बार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी को लेकर उच्च न्यायालयों ने सरकार को निर्देश दिए हैं। उदाहरण के तौर पर, 2019 में केंद्रीय सूचना आयोग के दो पदों की नियुक्ति में देरी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा था और इसे सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन बताया था।
निष्कर्ष
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक गंभीर समस्या है। इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सरकारी नीतियों में सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है, ताकि सूचना का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके और नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005)
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी पर एक संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए, हमें इस कानून के उद्देश्यों, इसकी प्रक्रियाओं और इसकी कार्यप्रणाली से जुड़ी सभी जानकारी को विस्तार से देखना होगा। इस संदर्भ में, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की देरी का प्रभाव इस अधिनियम की सफलता और कार्यप्रणाली पर पड़ता है।
1. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का परिचय
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारत में नागरिकों को सरकारी और सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।
इस कानून के तहत, किसी भी भारतीय नागरिक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
- सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- यदि किसी नागरिक को सूचना प्राप्त नहीं होती, तो उसकी अपील की प्रक्रिया होती है।
कानून के तहत नागरिकों को एक नियत प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जो पारदर्शिता और शासन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2. सूचना आयोग और सूचना आयुक्तों की भूमिका
सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC और State Information Commissions – SIC) उस तंत्र का हिस्सा है, जो सूचना के अधिकार की कार्यवाही और शिकायतों का निपटान करता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य है:
- शिकायतों का निवारण: जब किसी व्यक्ति को सूचना के लिए आवेदन करने पर उसकी जानकारी नहीं मिलती या उसे सही समय पर जानकारी नहीं मिलती, तो वह सूचना आयोग में अपील कर सकता है।
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय: सूचना आयुक्त किसी शिकायत पर निर्णय लेते हैं, यदि विभागीय अधिकारी द्वारा सूचना देने में कोई गलती की जाती है।
सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून में स्पष्ट प्रावधान हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में 10 आयुक्त हो सकते हैं, जिनमें एक केंद्रीय सूचना आयुक्त (CIC) होता है। राज्य सूचना आयोगों में भी इसी तरह की व्यवस्था होती है।
3. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय और राज्य स्तर पर विशेष प्रक्रिया द्वारा होती है।
- निर्धारित प्रक्रिया: सूचना आयुक्तों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, और विपक्षी नेता शामिल होते हैं।
- उम्मीदवार की योग्यताएँ: उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और सूचना के अधिकार के प्रति समर्पित होना चाहिए, और इसके लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों का चुनाव किया जाता है।
यह प्रक्रिया संविधान और संबंधित कानूनों के तहत सुनिश्चित की जाती है ताकि आयुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। लेकिन कई बार इसमें देरी होती है, जो कई कारणों से हो सकती है।
4. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी और RTI अधिनियम का प्रभाव
जब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी होती है, तो इसका सूचना के अधिकार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार किसी आयोग के माध्यम से ही मिलता है।
a) RTI कानून का उल्लंघन
सूचना आयोग के बिना शिकायतों और अपीलों का निपटान नहीं हो पाता। जब आयोग में पद रिक्त होते हैं, तो मामलों का समाधान नहीं हो पाता, और इससे RTI कानून का उल्लंघन होता है। यह नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है, क्योंकि वे अपनी शिकायतों का समाधान नहीं करवा पाते।
b) सरकारी पारदर्शिता पर असर
सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। यदि आयोग के पास पर्याप्त आयुक्त नहीं होते हैं, तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इससे सरकार की कार्यशैली और जनसुरक्षा पर असर पड़ता है।
c) समयबद्ध निपटान में कमी
सूचना आयोग की कार्यप्रणाली समयबद्ध होती है, यानी नागरिकों को उनकी शिकायतों का निपटान एक निश्चित समय सीमा के भीतर मिलना चाहिए। जब आयोग में रिक्तियां होती हैं, तो निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है और नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिलता।
5. RTI के तहत शिकायतों और अपीलों का निपटान
- पहला चरण: यदि कोई नागरिक सूचना के लिए आवेदन करता है और उसे सूचना नहीं मिलती, तो वह संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से जवाब की उम्मीद करता है।
- दूसरा चरण: यदि पहले चरण में समाधान नहीं होता, तो नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। इस शिकायत का निपटान सूचना आयुक्त करता है।
- तीसरा चरण: यदि शिकायतकर्ता को दूसरी बार भी समाधान नहीं मिलता, तो वह अपील कर सकता है और अंतिम समाधान सूचना आयोग से ही लिया जा सकता है।
6. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के कारण
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के कुछ प्रमुख कारण हैं:
- राजनीतिक हस्तक्षेप: चयन प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव और चुनावी कारणों से नियुक्ति में देरी हो सकती है।
- अन्य नियुक्तियों के लिए प्राथमिकता: सरकार की प्राथमिकताएं कुछ अन्य क्षेत्रों पर हो सकती हैं, जिससे सूचना आयोग में नियुक्तियां पीछे रह जाती हैं।
- न्यायिक प्रक्रिया: कभी-कभी नियुक्तियों के लिए न्यायालय में लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिससे नियुक्तियों में देरी हो जाती है।
7. कानूनी और न्यायिक हस्तक्षेप
कई बार न्यायालयों को भी सरकार को निर्देश देना पड़ता है कि नियुक्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए, क्योंकि इससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। भारत के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में सरकार से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में तेजी लाने का आदेश दिया है।
8. उपसंहार
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और इसे लागू करने में सूचना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी होती है, तो यह RTI कानून की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अत: सरकार को इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए उपाय अपनाने चाहिए, ताकि RTI कानून के उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकें और नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें।
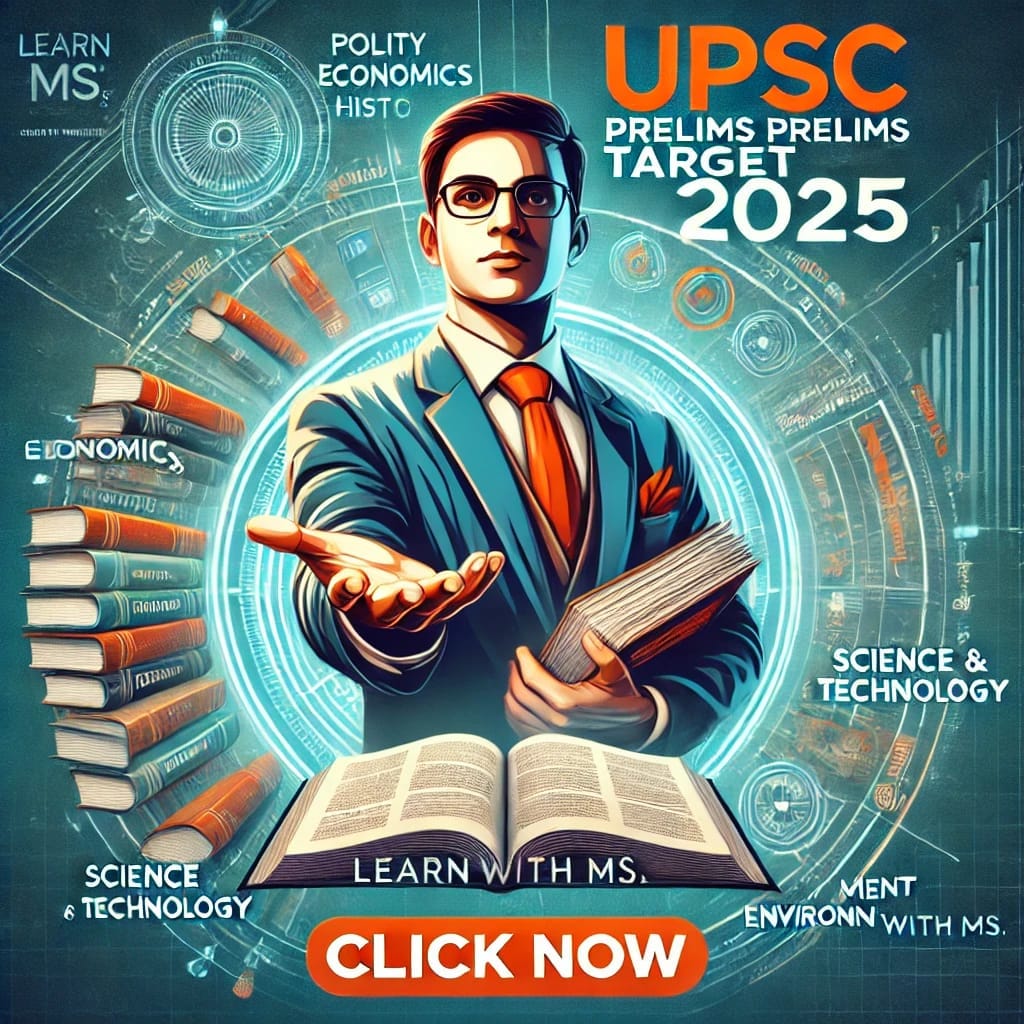
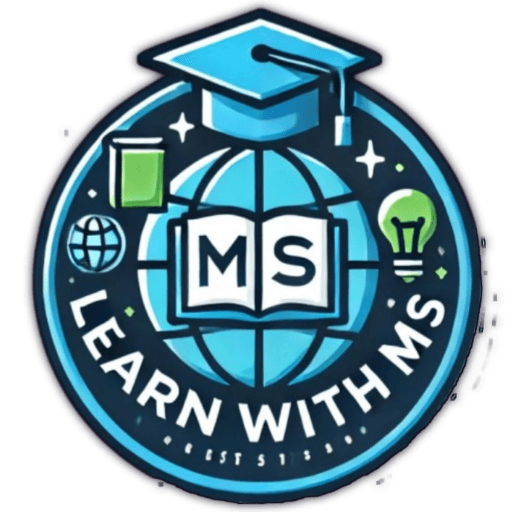
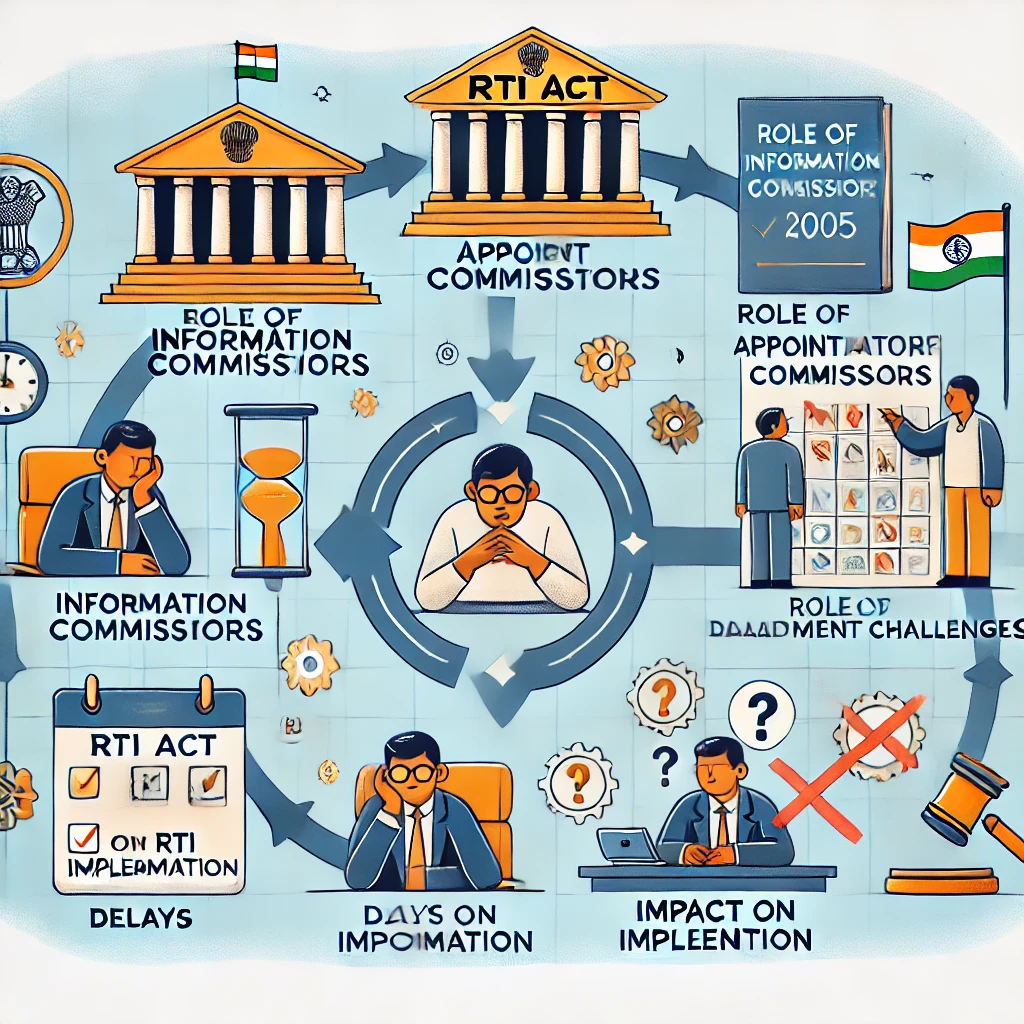
Leave a Reply