DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI FOR UPSC IAS – Prelims And Mains Examination 2025 | 22 JANUARY 2025 – UPSC PRELIMS POINTER Fact Based Current Affairs
DAILY Current Affairs Analysis For UPSC Pre And Mains Examination
Daily Archiveअदन की खाड़ी और लाल सागर ( Gulf of Aden and Red Sea )- UPSC Prelims Pointer
चर्चा में क्यों?
भारत के रक्षा मंत्री ने अदन की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीकी देशों के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती चुनौतियों, जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही, 2024 को ‘नौसेना नागरिक वर्ष’ (Naval Civilian Year) के रूप में मनाया गया, जो नौसेना के कार्यबल में नागरिक कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है।
समुद्री चुनौतियाँ और उनके प्रभाव
1. अदन की खाड़ी और लाल सागर के रणनीतिक महत्व:
- भौगोलिक स्थिति: अदन की खाड़ी और लाल सागर वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है।
- चोक प्वाइंट: बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच एक महत्वपूर्ण चोक प्वाइंट है, जो विश्व व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- भारत के लिए महत्व: भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। क्षेत्र में अस्थिरता से भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
2. समुद्री डकैती:
- सोमालियाई डकैती: सोमालिया के पास समुद्री डकैती ने 2000 के दशक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। हालाँकि, हाल के वर्षों में इसमें कमी आई है, लेकिन यह समस्या अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
- भारत पर प्रभाव: भारतीय व्यापारिक जहाज और मछुआरे इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं।
3. आतंकवाद और गैर-राज्य कृत्य:
- समुद्री मार्गों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के अवैध व्यापार के लिए किया जा सकता है।
- 26/11 का सबक: 2008 के मुंबई हमले ने दिखाया कि समुद्री मार्गों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कैसे किया जा सकता है।
4. क्षेत्रीय संघर्ष:
- यमन, सऊदी अरब और अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
- भविष्य की चुनौतियाँ: राजनीतिक अस्थिरता, पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री संघर्ष बढ़ सकते हैं।
भारत की नौसैनिक भूमिका
1. भारतीय नौसेना का दृष्टिकोण:
- मिशन SAGAR: Security and Growth for All in the Region का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- Operation Sankalp: यह ऑपरेशन अदन की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया।
- INS Vikramaditya और INS Vikrant: स्वदेशी विमानवाहक पोत भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाते हैं।
2. नौसेना और क्षेत्रीय सहयोग:
- IORA (Indian Ocean Rim Association): क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- मालाबार अभ्यास: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास।
- सागर मित्रता: हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में प्रयास।
3. ‘नौसेना नागरिक वर्ष’ का महत्व:
- भारतीय नौसेना के कार्यबल का लगभग एक तिहाई हिस्सा नागरिक कर्मचारियों का है।
- यह पहल उनके योगदान को मान्यता देने और उनके कौशल को और बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है।
समाधान और नीति सुझाव
- समुद्री सुरक्षा में निवेश:
- उन्नत पोत, ड्रोन और निगरानी प्रणाली का उपयोग।
- क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना:
- अदन की खाड़ी और लाल सागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- बहुपक्षीय नौसेना अभ्यासों में सक्रिय भागीदारी।
- डिजिटल और प्रौद्योगिकीय सुधार:
- समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए AI और GIS तकनीकों का उपयोग।
- बंदरगाहों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा उपाय।
- आर्थिक सहयोग:
- क्षेत्रीय देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
- सामरिक चोक प्वाइंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष
भारत के समुद्री हित और सुरक्षा रणनीति वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। अदन की खाड़ी और लाल सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की सक्रिय भागीदारी और नौसेना की उपस्थिति न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग में भी योगदान देगी।
‘नौसेना नागरिक वर्ष’ जैसे प्रयास भारत के नौसैनिक बल को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
UPSC दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न
1. मुख्य परीक्षा (GS-2 और GS-3):
- प्रश्न: भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति में भारतीय नौसेना की भूमिका पर चर्चा करें।
- प्रश्न: अदन की खाड़ी और लाल सागर के क्षेत्रीय संकट का भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव का विश्लेषण करें।
- प्रश्न: भारत के मिशन SAGAR का उद्देश्य और महत्व समझाएँ।
2. प्रीलिम्स संभावित प्रश्न:
- IORA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
- उत्तर: मॉरीशस।
- Operation Sankalp का संबंध किससे है?
- उत्तर: अदन की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा।
- नौसेना नागरिक वर्ष का उद्देश्य क्या है?
- उत्तर: नौसेना में नागरिक कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देना।
ISRO ने गगनयान के पहले बिना चालक मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल भेजा -Prelims Pointer
ISRO ने गगनयान के पहले बिना चालक मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल भेजा ( ISRO Dispatches Crew Module for the First Uncrewed Mission of Gaganyaan)
चर्चा में क्यों
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में गगनयान मिशन के पहले बिना चालक (Uncrewed) मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल (Crew Module) को सफलतापूर्वक भेजा। इस ऐतिहासिक कदम के साथ, ISRO भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, और इसका उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष में मानव भेजने वाली चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करना है।
गगनयान मिशन के बारे में मुख्य जानकारी:
- गगनयान मिशन: यह मिशन ISRO का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इसका उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने में सक्षम बनाना है, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर यात्रा करने के लिए तैयार हो।
- क्रू मॉड्यूल: गगनयान मिशन में शामिल क्रू मॉड्यूल मानव अंतरिक्ष यात्री के लिए आवश्यक सभी उपकरणों और प्रणालियों से लैस होगा, जो उन्हें अंतरिक्ष में जीवन और कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस मॉड्यूल में जीवन रक्षा प्रणाली, संचार उपकरण, और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण होंगे।
गगनयान मिशन के महत्व:
- भारत की अंतरिक्ष शक्ति में वृद्धि: गगनयान मिशन भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना देगा। यह भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख को भी मजबूत करेगा।
- तकनीकी विकास: इस मिशन के लिए आवश्यक तकनीक और प्रणाली भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी विकास की ओर इशारा करती है, जो भविष्य के अन्य मिशनों के लिए सहायक सिद्ध होगी।
- वैज्ञानिक अनुसंधान: गगनयान मिशन के दौरान विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाएंगे, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव शरीर पर प्रभाव और अन्य अंतरिक्ष से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन। यह अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल:
क्रू मॉड्यूल को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक हो। इसमें जीवन रक्षा प्रणाली, संचार उपकरण, और पूरे मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री की देखभाल करने के लिए सभी आवश्यक प्रौद्योगिकियाँ होंगी। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में सुरक्षा, नियंत्रण और जीवन को बनाए रखना है।
मिशन के चरण:
- बिना चालक मिशन: गगनयान मिशन का पहला चरण बिना चालक मिशन के रूप में होगा, जिसमें क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रणालियाँ ठीक से काम कर रही हैं। यह मिशन मुख्य रूप से सिस्टम और सुरक्षा परीक्षण के रूप में कार्य करेगा।
- चालक मिशन: बिना चालक मिशन की सफलता के बाद, अगले चरण में मानव अंतरिक्ष यात्री को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन मानव अंतरिक्ष यात्री के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा।
ISRO द्वारा उठाए गए कदम:
- प्रौद्योगिकी का विकास: ISRO ने गगनयान मिशन के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास किया है, जैसे कि क्रू मॉड्यूल, जीवन रक्षा प्रणाली, और सुरक्षा उपकरण, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- प्रशिक्षण: भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जो उन्हें अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी में मदद करेगा। प्रशिक्षण में शारीरिक, मानसिक और तकनीकी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सम्भावित चुनौतियाँ:
- सुरक्षा: अंतरिक्ष यात्रा में सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती है। ISRO को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रू मॉड्यूल और अन्य प्रणालियाँ पूरी तरह से सुरक्षित हों।
- तकनीकी परीक्षण: बिना चालक मिशन के दौरान किए गए सभी परीक्षणों की सफलता गगनयान मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी।
निष्कर्ष:
गगनयान मिशन ISRO के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, और इसका उद्देश्य भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर स्थापित करना है। क्रू मॉड्यूल का सफल प्रक्षेपण मिशन की सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नई ऊँचाई की ओर अग्रसर होने का संकेत है।
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (ASSET RECONSTRUCTION COMPANIES -ARC)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से संबंधित दिशानिर्देशों का संशोधन – विश्लेषण
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। एआरसी का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को पुनर्निर्मित करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम करना है। एआरसी द्वारा नकारात्मक परिसंपत्तियों (NPA) के समाधान से बैंकों के लिए वित्तीय संकट को कम करने में मदद मिलती है और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में सुधार होता है।
एआरसी का कार्य और महत्व:
एआरसी एक विशेष प्रकार की कंपनी है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) या बिगड़े हुए कर्ज खरीदती है और उनका पुनर्निर्माण करती है। एआरसी इन NPA को पुनर्निर्मित करके पुनः संपत्ति के मूल्य को सुधारने और कर्ज के भुगतान की प्रक्रिया को सक्षम बनाने का कार्य करती है। यह बैंकों को वित्तीय संकट से उबारने और उनके बैलेंस शीट को स्थिर करने में मदद करती है।
आरबीआई द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य:
- संचालन में पारदर्शिता और स्थिरता: आरबीआई ने एआरसी के संचालन में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इससे एआरसी को लेकर निवेशकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में विश्वास बनेगा, और यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सशक्त बनाएगा।
- पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना: नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य एआरसी के लिए पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है। इससे एआरसी को NPA समाधान के लिए नए तरीके अपनाने का अवसर मिलेगा, और उनके लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया संभव हो सकेगी।
- संसाधनों का बेहतर उपयोग: संशोधित दिशानिर्देशों में एआरसी को बेहतर संसाधनों के उपयोग की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इसमें उनके पास अधिक वित्तीय साधनों का उपयोग करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने, और निवेशकों को आकर्षित करने के उपाय शामिल हैं। यह बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- नियामक ढांचे को मजबूत करना: नए दिशानिर्देशों में एआरसी के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इससे एआरसी की गतिविधियों पर निगरानी रखने की प्रक्रिया सख्त हो जाएगी और वे अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।
- गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण: एआरसी के लिए दिशानिर्देशों में सुधार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया गुणवत्ता और अनुशासन के साथ की जा रही हो। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए उधारी की वसूली में सुधार होगा।
संशोधित दिशानिर्देशों के मुख्य पहलू:
- एनपीए खरीदने के तरीके: एआरसी के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में, अब वे अधिकतम एनपीए को खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह उनकी क्षमता को बढ़ाएगा और बैंकों से बिगड़े हुए कर्ज को तेजी से खरीदने की सुविधा देगा।
- नवीनतम पुनर्निर्माण प्रक्रिया: नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एआरसी अब अधिक लचीला और प्रभावी तरीके से पुनर्निर्माण प्रक्रिया को लागू कर सकेंगे। इसमें अतिरिक्त वित्तीय साधनों का उपयोग करने की अनुमति होगी, जैसे कि लोन से ज्यादा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- संपत्ति का पुनर्निर्माण: एआरसी को अब संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए एक विस्तृत और कार्यकुशल योजना बनाने की आवश्यकता होगी। यह योजना संपत्ति के मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
- प्रवर्तन और निगरानी: नए दिशानिर्देशों के तहत, आरबीआई एआरसी की गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एआरसी अपने काम में अनुशासन बनाए रखें और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य को पूरा करें।
सारफेसी अधिनियम और संशोधित आरबीआई दिशानिर्देशों का संबंध:
- नियामक ढांचे में सुधार: संशोधित आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत, एआरसी के लिए निर्धारित कार्यशैली और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए गए हैं। इसके माध्यम से एआरसी अधिक जिम्मेदारी के साथ कर्ज वसूली की प्रक्रिया का पालन करेंगे, जो कि SARFAESI अधिनियम के तहत पहले से निर्धारित अधिकारों और जिम्मेदारियों के अनुरूप होगा।
- संपत्ति वसूली में तेज़ी: सारफेसी अधिनियम के तहत एआरसी को संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने का अधिकार है, जो समयबद्ध और अधिक प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है। संशोधित दिशानिर्देश एआरसी को इस प्रक्रिया में अधिक संसाधन और लचीलापन प्रदान करते हैं।
- पारदर्शिता और निगरानी: एआरसी के लिए आरबीआई द्वारा संशोधित दिशानिर्देश एआरसी के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करते हैं, जिससे SARFAESI अधिनियम के तहत संपत्ति वसूली की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है।
- नए वित्तीय साधनों का उपयोग: संशोधित दिशानिर्देशों में एआरसी को नए वित्तीय साधनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जैसे कि बेहतर पुनर्निर्माण योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधनों का इस्तेमाल। यह SARFAESI अधिनियम के तहत संपत्तियों की वसूली और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है।
आरबीआई के कदम के लाभ:
- बैंकिंग सिस्टम में सुधार: संशोधित दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप, बैंकों के पास अधिक समय और संसाधन होंगे NPA के समाधान के लिए। इससे बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- अर्थव्यवस्था को लाभ: जब एआरसी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के खराब कर्ज को निपटाने में सक्षम होंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बैंकों में सुधार होने से वित्तीय संस्थाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे और इससे विकास में गति आएगी।
- निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा: अधिक पारदर्शिता, स्थिरता, और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से एआरसी के काम में सुधार होगा, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। यह देश में विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करेगा।
- नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स का समाधान: एआरसी के साथ अधिक प्रभावी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स का समाधान संभव होगा। इससे बैंकों का NPA कम होगा और उनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी।
- नई कारोबारी संभावनाएँ: नई नीतियों के परिणामस्वरूप, एआरसी के लिए नए कारोबारी अवसर उत्पन्न होंगे। इसका प्रभाव न केवल बैंकों पर पड़ेगा, बल्कि देशभर के व्यापारिक क्षेत्रों में भी होगा।
संभावित चुनौतियाँ:
- संपत्ति की सही मूल्यांकन: एआरसी को एनपीए संपत्तियों का सही मूल्यांकन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सही मूल्यांकन न होने पर, पुनर्निर्माण में कठिनाइयाँ आ सकती हैं।
- बैंकों का सहयोग: एआरसी को बैंकों के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा, जिससे बैंकिंग संस्थानों का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- नियामक ढांचे में सुधार की आवश्यकता: जबकि आरबीआई ने सुधार किए हैं, फिर भी एआरसी के कार्यों की निगरानी में और सुधार की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं।
निष्कर्ष:
आरबीआई द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम बैंकों के लिए नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के समाधान को आसान बनाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में चुनौतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन यदि सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक स्थिर और प्रतिस्पर्धात्मक बना सकता है।
स्वामित्व योजना (SVAMITVA SCHEME)
चर्चा में क्यों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया कि केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत, जब देश के सभी गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे, तो इससे 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रस्तुत स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण की घोषणा, ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कानूनी अधिकार प्रदान करने का कार्य करेगी और इससे न केवल व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों को स्पष्टता मिलेगी, बल्कि इससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए, हम इस योजना का विस्तृत विश्लेषण करते हैं:
पृष्ठभूमि: –
- प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों के संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य
स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति से संबंधित अधिकारों को कानूनी रूप से स्पष्ट करना है। इसके तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के मालिक होने का अधिकार दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके पास संपत्ति का वैध दस्तावेज हो। इससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।
संपत्ति कार्ड का वितरण:
स्वामित्व योजना के तहत, संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे, जो कि ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के अधिकार का कानूनी प्रमाण प्रदान करेंगे। यह कार्ड एक तरह से संपत्ति के दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा, जिसे लोग अपनी संपत्ति को प्रमाणित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके वितरण से ग्रामीणों के पास संपत्ति के मालिकाना हक का स्पष्ट दस्तावेज होगा, जो उन्हें वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि:
प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के संदर्भ में यह कहा कि जब संपत्ति कार्ड पूरे देश के गांवों में वितरित हो जाएंगे, तो इससे 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि जब ग्रामीणों के पास अपने संपत्ति का कानूनी प्रमाण होगा, तो वे अपने संपत्ति का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। यह उन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने, व्यवसाय शुरू करने और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्षम बनाएगा।
स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड मिलने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, बल्कि यह छोटे व्यापारियों, किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आएगी और अधिक व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू हो सकेंगी।
आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल सुधार:
इस योजना का एक अन्य प्रमुख लाभ यह होगा कि यह ग्रामीण भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएगा। संपत्ति कार्डों का वितरण डिजिटल रूप से होगा, जिससे डिजिटल साक्षरता और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, यह योजना ग्रामीण भारत में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को भी सशक्त बनाएगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
स्वामित्व योजना के लाभ:
- संपत्ति अधिकारों का प्रमाणीकरण: ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिलेगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी और संपत्ति का सही मालिक पहचान में आएगा।
- वित्तीय समावेशन: संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीण लोग अब वित्तीय संस्थाओं से लोन प्राप्त कर सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था। यह उन्हें उद्यमिता और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए सक्षम बनाएगा।
- स्थानीय विकास: जब लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे, तो इससे व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय बाजारों में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- डिजिटल साक्षरता में वृद्धि: यह योजना ग्रामीणों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे डिजिटल साक्षरता में वृद्धि होगी।
- भूमि सुधार: यह योजना भूमि सुधारों को भी बढ़ावा देगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
संभावित चुनौतियाँ:
- डिजिटल साक्षरता की कमी: जबकि यह योजना डिजिटल तरीके से लागू होगी, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की धीमी गति और डिजिटल साक्षरता की कमी हो सकती है, जिससे योजना का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- संपत्ति दस्तावेजों की गलतियों और विवाद: कुछ क्षेत्रों में भूमि दस्तावेजों में गलतियाँ हो सकती हैं, जिनका समाधान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में भूमि विवाद हो सकते हैं, जिन्हें हल करना समय-साध्य हो सकता है।
- प्रभावी कार्यान्वयन: इस योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन और सभी गांवों तक संपत्ति कार्ड की पहुँच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर उन गांवों में जहाँ प्रशासनिक प्रणाली और संसाधनों की कमी है।
निष्कर्ष:
स्वामित्व योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह न केवल संपत्ति अधिकारों की पुष्टि करेगी, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इसे लागू करने में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन यदि सही तरीके से लागू किया गया तो यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
तमिलनाडु के समुद्र तटों पर मृत ऑलिव रिडले कछुए ( OLIVE RIDLEY TURTLES )
तमिलनाडु के समुद्र तटों पर मृत ऑलिव रिडले कछुए: कारण और विश्लेषण
प्रसंग:
पिछले दो सप्ताह में तमिलनाडु, विशेषकर चेन्नई के समुद्र तटों पर बड़ी संख्या में मृत ऑलिव रिडले कछुए (Olive Ridley Turtles) पाए गए हैं। यह घटना न केवल पर्यावरणीय संकट को उजागर करती है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है।
ऑलिव रिडले कछुए के बारे में मुख्य तथ्य:
- वैज्ञानिक नाम: Lepidochelys olivacea
- स्थिति:
- IUCN (International Union for Conservation of Nature): असुरक्षित (Vulnerable)
- भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित।
- प्राकृतिक निवास: उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्र।
- प्रजनन:
- “अरिबाडा” प्रक्रिया: जब हजारों कछुए एक साथ अंडे देने के लिए समुद्र तटों पर आते हैं।
- भारत में ओडिशा का गहिरमाथा समुद्र तट उनका प्रमुख प्रजनन स्थल है।
मृत कछुओं की घटनाओं के प्रमुख कारण:
1. मछली पकड़ने की गतिविधियाँ:
- गैर-पारंपरिक मछली पकड़ने के जाल:
- कछुए अक्सर ट्रॉलर और मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं।
- सांस लेने में असमर्थता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है।
- TEDs (Turtle Excluder Devices):
- ट्रॉलर में इन उपकरणों का उपयोग पर्याप्त नहीं है।
- इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा।
2. प्रदूषण:
- समुद्री प्लास्टिक कचरा:
- प्लास्टिक कचरे को खाने से कछुओं का पाचन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है।
- रासायनिक प्रदूषण:
- औद्योगिक अपशिष्ट और तेल रिसाव के कारण समुद्री जल की गुणवत्ता खराब होती है।
3. जलवायु परिवर्तन:
- समुद्र का तापमान:
- समुद्र के बढ़ते तापमान से प्रजनन स्थान प्रभावित होते हैं।
- समुद्र स्तर में वृद्धि:
- उनके प्राकृतिक घोंसले समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ गया है।
4. प्रकाश प्रदूषण:
- समुद्र तटों पर बढ़ते शहरीकरण और प्रकाश के कारण कछुए दिशाभ्रम का शिकार हो जाते हैं।
5. प्राकृतिक शिकारी:
- समुद्र तट पर अंडे और छोटे कछुए प्राकृतिक शिकारियों का शिकार हो जाते हैं।
इस घटना का पर्यावरणीय प्रभाव:
- पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:
- कछुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- मृत कछुओं की संख्या में वृद्धि से समुद्र तटीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है।
- जैव विविधता का नुकसान:
- कछुए की मृत्यु समुद्र की जैव विविधता को प्रभावित करती है।
- पर्यावरणीय चेतावनी:
- यह घटना समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर चेतावनी है।
सरकार और संगठन की भूमिका:
1. वर्तमान कानून और उपाय:
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:
ऑलिव रिडले कछुओं को शेड्यूल I के तहत संरक्षित किया गया है। - सीआरजेड (CRZ) विनियम:
- तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए हैं।
- तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है।
- TEDs का उपयोग अनिवार्य:
- ट्रॉलरों में कछुए बचाने के उपकरण (TEDs) लगाना अनिवार्य है।
2. संरक्षण कार्यक्रम:
- ओडिशा का कछुआ संरक्षण:
- गहिरमाथा समुद्र तट पर सक्रिय संरक्षण प्रयास।
- NGOs और स्थानीय संगठनों की भूमिका:
- तमिलनाडु और अन्य राज्यों में जागरूकता अभियान चलाना।
समाधान और सुधार के उपाय:
1. मछली पकड़ने की प्रथाओं में सुधार:
- TEDs के उपयोग को सख्ती से लागू करें।
- अनधिकृत मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगाएं।
2. प्रदूषण नियंत्रण:
- समुद्र में प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं।
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भारी जुर्माना लगाएं।
3. संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग:
- जीपीएस ट्रैकिंग:
- कछुओं की आवाजाही और प्रजनन स्थलों की निगरानी।
- जैव विविधता डेटा संग्रहण:
- समुद्री जीवन पर प्रभाव का अध्ययन।
4. सामुदायिक जागरूकता:
- स्थानीय मछुआरों और निवासियों को कछुओं के महत्व और संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित करें।
- समुद्र तट की सफाई के लिए नियमित अभियान।
5. अनुसंधान और विकास:
- कछुओं के प्रजनन और उनके प्रवास पर शोध।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियाँ।
निष्कर्ष:
ऑलिव रिडले कछुए पर्यावरण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु के समुद्र तटों पर बड़ी संख्या में कछुओं की मौत पर्यावरणीय असंतुलन और मानवीय गतिविधियों का नतीजा है।
सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। कछुओं की रक्षा न केवल एक प्रजाति को बचाने का प्रयास है, बल्कि यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने की जिम्मेदारी भी है।
भारत का आर्थिक धीमापन और जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 : India’s Economic Slowdown and GDP Growth Rate 2024-25
परिचय
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर 6.4% होने का अनुमान दिया है। यह पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। इसके पीछे घरेलू और वैश्विक कारणों का प्रभाव है।
प्रमुख आंकड़े और तथ्य:
| विवरण | आंकड़ा | पिछला वर्ष (2023-24) |
|---|---|---|
| जीडीपी वृद्धि दर | 6.4% | 7.2% |
| कृषि क्षेत्र वृद्धि दर | 3.5% | 3.9% |
| औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि दर | 5.2% | 5.8% |
| सेवा क्षेत्र वृद्धि दर | 7.3% | 9.1% |
| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) | 5.4% (औसत) | 5.8% |
गिरावट के कारण:
1. घरेलू कारण
- मुद्रास्फीति:
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।
- मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति में कमी।
- ब्याज दरों में वृद्धि:
- आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया, जिससे निवेश और खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- रोजगार में कमी:
- औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन धीमा।
2. वैश्विक कारण
- वैश्विक आर्थिक मंदी:
- अमेरिका, यूरोप और चीन की धीमी आर्थिक प्रगति ने भारतीय निर्यात को प्रभावित किया।
- यूक्रेन-रूस संघर्ष:
- ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान।
- विनिमय दर:
- भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, जिससे आयात महंगा हो गया।
आर्थिक मंदी के प्रमुख संकेतक
| संकेतक | 2024-25 | 2023-24 | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| जीडीपी वृद्धि दर | 6.4% | 7.2% | चार वर्षों में सबसे कम। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती। |
| कृषि वृद्धि दर | 3.5% | 3.9% | जलवायु परिवर्तन और असमान मानसून का प्रभाव। |
| औद्योगिक वृद्धि दर | 5.2% | 5.8% | निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट। |
| सेवा क्षेत्र वृद्धि दर | 7.3% | 9.1% | वित्तीय और आईटी सेवाओं में सुस्ती। |
| महंगाई दर (CPI) | 5.4% | 5.8% | उपभोक्ता खर्च में गिरावट। |
क्षेत्रीय योगदान और विश्लेषण
| क्षेत्र | वृद्धि दर (2024-25) | मुख्य कारण |
|---|---|---|
| कृषि | 3.5% | असमान वर्षा, जलवायु परिवर्तन और कम उत्पादकता। |
| उद्योग | 5.2% | मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण में गिरावट। |
| सेवा | 7.3% | यात्रा और पर्यटन में वृद्धि, लेकिन वित्तीय सेवाओं में सुस्ती। |
सकारात्मक पहलू:
- सरकारी निवेश:
- ₹10 लाख करोड़ से अधिक का बुनियादी ढांचे में निवेश।
- डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत नई योजनाएँ।
- विदेशी निवेश:
- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने $75 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया।
- सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप्स में बढ़ती रुचि।
- हरित ऊर्जा:
- सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी।
संभावित प्रभाव:
| क्षेत्र | प्रभाव |
|---|---|
| उपभोक्ता | उच्च मुद्रास्फीति के कारण घरेलू बजट पर दबाव। |
| व्यवसाय | उच्च ब्याज दरों के कारण कर्ज महंगा, निवेश धीमा। |
| सरकार | राजकोषीय घाटा नियंत्रण करना चुनौतीपूर्ण। |
| रोजगार | सेवा क्षेत्र में कुछ सुधार, लेकिन समग्र रोजगार वृद्धि धीमी। |
आगे की राह:
1. संरचनात्मक सुधार
- मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को प्रोत्साहन।
- कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार।
2. कृषि सुधार
- जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना।
- किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता।
3. वैश्विक व्यापार
- निर्यात बाजार का विविधीकरण।
- ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करना।
4. सरकारी नीतियाँ
- बुनियादी ढाँचे और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश।
- रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन।
निष्कर्ष:
भारत की 2024-25 की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट अल्पकालिक चुनौतियों का परिणाम है। हालांकि, मजबूत नीतियों और निवेश योजनाओं से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाएँ प्रबल हैं। भारत को घरेलू सुधारों और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।
गौरतलब है कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता अभी भी मजबूत बनी हुई है, और सही दिशा में कदम उठाने से यह गति वापस प्राप्त कर सकता है।
चुनावी ट्रस्ट और राजनीतिक दान : Electoral Trust and Political Donation:
चुनावी ट्रस्ट और राजनीतिक दान :
पृष्ठभूमि:
चुनावी बांड और चुनावी ट्रस्ट दोनों का उद्देश्य राजनीतिक दलों को पारदर्शिता के साथ वित्तीय योगदान देना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड को समाप्त करने के निर्णय के बाद चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से दान में वृद्धि हुई है।
चुनावी ट्रस्ट क्या हैं?
चुनावी ट्रस्ट गैर-लाभकारी संस्थाएं होती हैं जिन्हें भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दान को एकत्रित करके इसे राजनीतिक दलों को पारदर्शी तरीके से वितरित करना है।
भारत में चुनावी दान के आंकड़े:
- वृद्धि:
- चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से दान में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- अधिकांश दान प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों और उद्यमियों से आया है।
- पारदर्शिता:
- चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से दिया गया दान सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया जाता है, जिससे यह चुनावी बांड की तुलना में अधिक पारदर्शी है।
- प्रमुख दल:
- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस को सबसे अधिक दान मिला।
- क्षेत्रीय दलों को भी दान में वृद्धि हुई है, लेकिन राष्ट्रीय दलों की तुलना में उनकी हिस्सेदारी कम है।
चुनावी ट्रस्ट के लाभ:
- पारदर्शिता:
- चुनावी बांड की गोपनीयता के विपरीत, चुनावी ट्रस्ट दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के नाम का खुलासा करते हैं।
- वित्तीय योगदान का केंद्रीकरण:
- कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दानदाताओं के लिए यह एक सरल माध्यम है।
- कानूनी संरक्षण:
- भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों और नियमों के तहत कार्य करते हैं।
कानूनी ढांचा और विश्लेषण
1. चुनावी ट्रस्ट: कानूनी आधार
चुनावी ट्रस्ट भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं। इनका गठन दान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है।
प्रमुख कानूनी प्रावधान:
- कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013)
- धारा 8:
चुनावी ट्रस्ट गैर-लाभकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होते हैं। - कंपनियों के लिए दिशानिर्देश:
कंपनियां अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 7.5% तक राजनीतिक दान में दे सकती हैं।
(पहले 5% की सीमा थी, जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत बढ़ाया गया।)
- धारा 8:
- आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961)
- धारा 13A:
राजनीतिक दलों को चुनावी ट्रस्टों से प्राप्त दान पर आयकर से छूट मिलती है। - धारा 80GGB और 80GGC:
कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दानदाताओं को चुनावी ट्रस्ट को दान पर कर छूट मिलती है।
- धारा 13A:
- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)
- निर्देश संख्या:
चुनावी ट्रस्टों को दान और वितरण का पूर्ण विवरण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास जमा करना होता है। - दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने का प्रावधान।
- निर्देश संख्या:
- चुनावी बांड और पारदर्शिता
- चुनावी बांड योजना, 2018:
इसे चुनावी ट्रस्ट से पहले पारदर्शी दान का माध्यम माना गया, लेकिन इसमें गोपनीयता की आलोचना हुई। - सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में चुनावी बांड को समाप्त कर दिया, जिससे ट्रस्टों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई।
- चुनावी बांड योजना, 2018:
2. कानूनी मुद्दे और चुनौतियाँ
- पारदर्शिता की सीमा:
- चुनावी ट्रस्ट दानदाताओं और राजनीतिक दलों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती कि ये दान किन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए।
- केंद्र सरकार का प्रभाव:
- बड़े कॉर्पोरेट दान का एक बड़ा हिस्सा सत्ता में रहने वाले दलों को मिलता है, जिससे विपक्ष और छोटे दलों के लिए असमानता बढ़ती है।
- कॉर्पोरेट शासन का प्रभाव:
- कंपनियां राजनीतिक दान के माध्यम से नीतिगत फैसलों पर प्रभाव डाल सकती हैं, जो नीति निर्माण में पारदर्शिता के विपरीत है।
3. सुधार के उपाय (कानूनी दृष्टिकोण)
- कानूनी सुधार:
- निर्वाचन सुधार समिति की सिफारिशें लागू करें।
- राजनीतिक दलों को प्राप्त सभी दानों का विवरण सार्वजनिक करने का अनिवार्य प्रावधान।
- पारदर्शिता का विस्तार:
- चुनावी ट्रस्टों द्वारा राजनीतिक दलों को किए गए दान की सार्वजनिक ऑडिट।
- दान और उसके उपयोग के उद्देश्य को चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाए।
- समान वित्तीय अवसर:
- धारा 80GGC के तहत क्षेत्रीय दलों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कर छूट का प्रावधान।
- स्वतंत्र संस्था की स्थापना:
- चुनावी दान और खर्च पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाए।
- डिजिटल रजिस्टर:
- डिजिटल ट्रांसपेरेंसी रजिस्टर: जिसमें चुनावी ट्रस्टों और दानदाताओं का वास्तविक समय में विवरण उपलब्ध हो।
4. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और इसका प्रभाव
- निर्णय का सार:
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” ठहराया और इसे समाप्त कर दिया।
- न्यायालय ने पारदर्शिता की कमी और चुनावी वित्तपोषण में असंतुलन को इसका आधार बनाया।
- परिणाम:
- चुनावी ट्रस्ट अब पारदर्शिता के लिए एकमात्र बड़ा विकल्प बन गए हैं।
- राजनीतिक दान में वृद्धि हुई, लेकिन छोटे दलों को अभी भी उचित भागीदारी नहीं मिल रही।
चुनौतियाँ:
- सत्ता का केंद्रीकरण:
- अधिकांश दान प्रमुख राजनीतिक दलों को मिलता है, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दलों को प्रतिस्पर्धा में मुश्किल होती है।
- कॉर्पोरेट प्रभाव:
- बड़े कॉर्पोरेट दानदाताओं के कारण राजनीतिक निर्णयों पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है।
- पारदर्शिता का आंशिक दायरा:
- दानदाताओं के नाम उजागर होते हैं, लेकिन यह पता लगाना कठिन है कि दान किन उद्देश्यों के लिए किया गया।
आगे की राह:
- पारदर्शी प्रणाली का निर्माण:
- चुनावी दान के स्रोतों और उपयोग को सार्वजनिक करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए।
- समानता की गारंटी:
- छोटे और क्षेत्रीय दलों को वित्तीय सहायता के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।
- स्वतंत्र ऑडिट:
- चुनावी ट्रस्ट और राजनीतिक दलों के वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा नियमित ऑडिट की आवश्यकता है।
निष्कर्ष:
चुनावी बांड के समाप्त होने के बाद चुनावी ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरे हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस प्रणाली का दुरुपयोग न हो और राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता बनी रहे। भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर सुधार और निगरानी की आवश्यकता है।
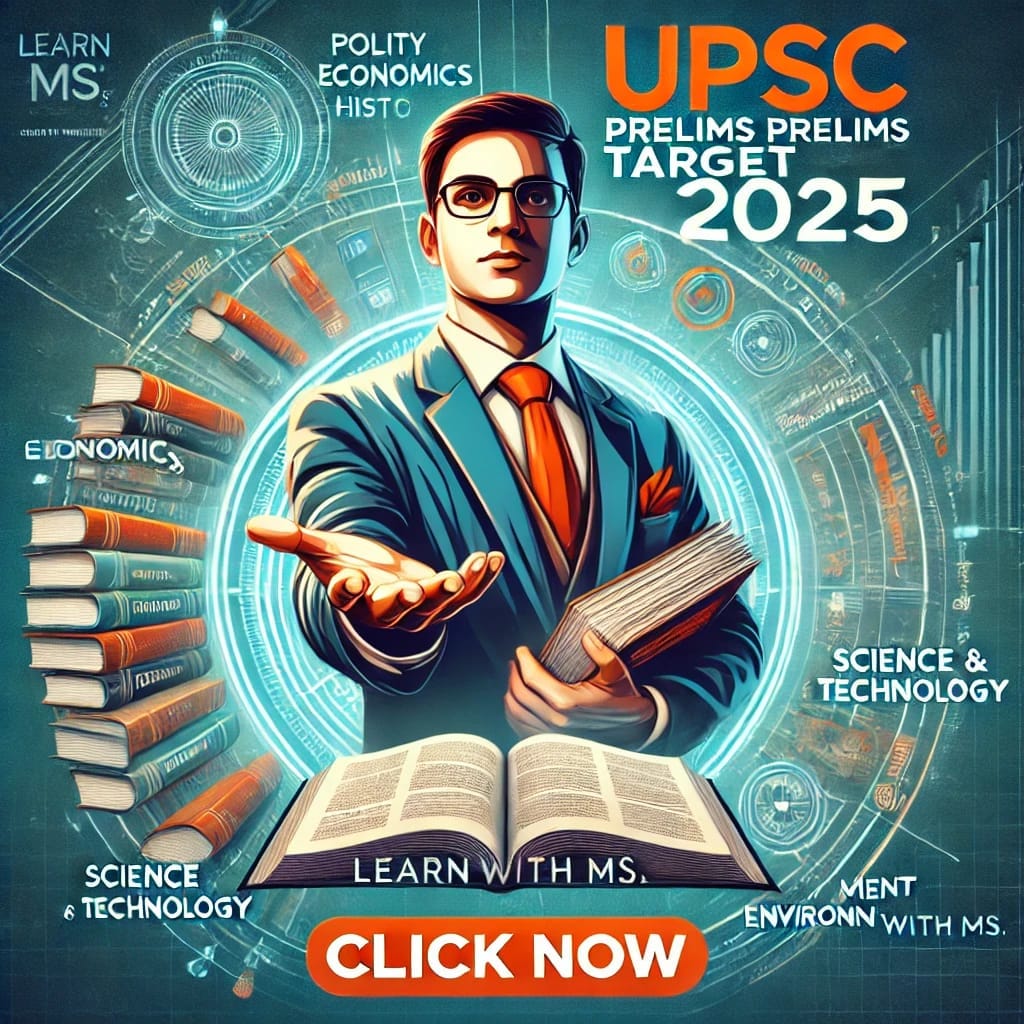
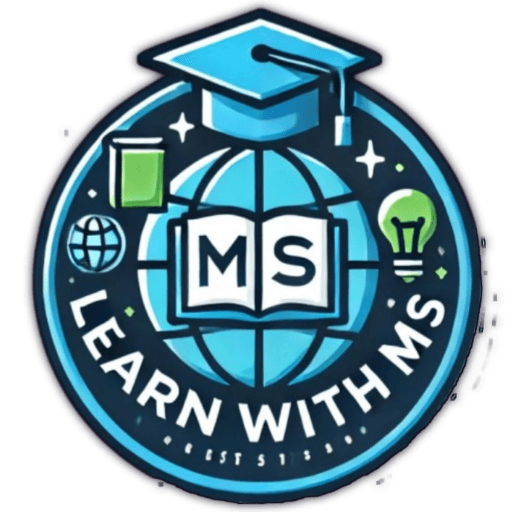
Leave a Reply