- चर्चा में क्यों?
- रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
- समाधान के उपाय:
- 1. शिक्षा की असमानता:
- 2. कुपोषण:
- 3. बाल श्रम:
- 4. बाल विवाह:
- 5. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी:
- 6. सामाजिक असमानता और भेदभाव:
- 7. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट:
- 8. मानसिक स्वास्थ्य:
- 9. सुरक्षा और हिंसा:
- 10. सड़क दुर्घटनाएँ और शारीरिक सुरक्षा:
- 1. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RCH):
- 2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:
- 3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):
- 4. मिड-डे मील योजना:
- 5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):
- 6. पोषण अभियान (Poshan Abhiyaan):
- 7. राजीव गांधी शिक्षा मिशन (Sarva Shiksha Abhiyan):
- 8. बाल श्रम निषेध योजना:
- 9. नैतिक शिक्षा और बाल सुरक्षा योजना:
- 10. जन्म से मृत्यु तक स्वास्थ्य देखभाल योजना (National Health Mission):
- 11. मूलभूत बालक शिक्षा योजना (Child Labour Projects):
- 12. आधार योजना:
- 13. मुख्यमंत्री बाल विकास योजना:
- 1. शिक्षा और कौशल विकास में सुधार:
- 2. कुपोषण से निपटने के लिए प्रभावी उपाय:
- 3. बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करना:
- 4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुधार:
- 5. बाल अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा:
- 6. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से निपटना:
- 7. संवेदनशील नीति और योजनाओं का विकास:
- 8. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार:
- निष्कर्ष:
चर्चा में क्यों?
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट “वर्ष 2025 में बच्चों के लिये संभावनाएँ: बच्चों के भविष्य के लिये लचीली प्रणालियों का निर्माण” जारी की है। इसमें बच्चों पर वैश्विक संकटों के बढ़ते प्रभावों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। यह रिपोर्ट बच्चों के कल्याण और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक उपायों को रेखांकित करती है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
- वैश्विक संकटों का प्रभाव:
- जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता, महामारी और युद्ध जैसे संकट बच्चों के जीवन और विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
- 1.3 अरब से अधिक बच्चे गरीबी, भूख, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य:
- शिक्षा में बाधा: COVID-19 के बाद 40% से अधिक बच्चों की शिक्षा अस्थिर हुई है।
- पोषण की समस्या: दुनिया भर में 45 मिलियन बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं।
- जलवायु संकट का असर:
- लगभग 1 अरब बच्चे उन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां जलवायु संबंधी संकट गहरा रहे हैं।
- पानी की कमी और बढ़ते तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- लचीली प्रणालियों की आवश्यकता:
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
- वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है ताकि सभी बच्चों के अधिकार सुरक्षित हो सकें।
समाधान के उपाय:
- निवेश और सुधार:
बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिये संसाधन बढ़ाने का सुझाव। - जलवायु अनुकूलन रणनीति:
बच्चों को जलवायु संकटों से बचाने के लिये विशेष योजनाएँ बनाना। - वैश्विक सहयोग:
यूनिसेफ ने सभी देशों से अपील की है कि वे बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दें और उन्हें संकटों से बचाने के लिये सामूहिक कदम उठाएँ।
समकालीन भारत में बच्चों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:
भारत में बच्चों को समृद्ध और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ उनके विकास और कल्याण के रास्ते में अड़चनें पैदा करती हैं। निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
1. शिक्षा की असमानता:
- प्रारंभिक शिक्षा का अभाव: देश के कई हिस्सों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों की कमी, खराब बुनियादी सुविधाएँ और शिक्षक कमी की समस्या है।
- शिक्षा का भेदभाव: बच्चों के बीच शिक्षा का असमान वितरण भी एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर महिला बच्चों, आदिवासी समुदाय और अन्य वंचित वर्गों के लिए।
- ऑनलाइन शिक्षा की बाधाएँ: COVID-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ, लेकिन इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल उपकरणों की कमी बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई।
2. कुपोषण:
- भारत में बच्चों के कुपोषण की दर बहुत उच्च है। हर साल लाखों बच्चे कुपोषण के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। कुपोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है।
- भारत में लगभग 45 मिलियन बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं, जो उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास में बाधक बनते हैं।
3. बाल श्रम:
- भारत में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है, जहाँ लाखों बच्चे घरेलू कामों, खेतों, कारखानों और सड़क पर काम करने के लिए मजबूर हैं। यह उन्हें शिक्षा से वंचित रखता है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है।
- हालाँकि बाल श्रम के खिलाफ कानूनी उपाय हैं, फिर भी सामाजिक-आर्थिक कारणों से यह समस्या बनी हुई है।
4. बाल विवाह:
- बाल विवाह भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। यह बच्चों के जीवन में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षति पहुँचाता है।
- बाल विवाह से किशोरी लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है।
5. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी:
- भारत में बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और महंगी स्वास्थ्य सेवाएँ बच्चों की देखभाल में रुकावट डालती हैं।
- टीकाकरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा की कमी भी बच्चों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।
6. सामाजिक असमानता और भेदभाव:
- भारत में जाति, धर्म, लिंग, और आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों में भेदभाव होता है, जिससे उनका समग्र विकास प्रभावित होता है।
- दलित, आदिवासी और मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और पोषण के अवसरों में असमानता का सामना करना पड़ता है।
7. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट:
- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे बाढ़, सूखा, और चक्रवात, बच्चों के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं।
- पर्यावरणीय संकट बच्चों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और भविष्य को प्रभावित करता है।
8. मानसिक स्वास्थ्य:
- बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती संख्या, जैसे अवसाद, चिंता, और तनाव, एक चिंता का विषय बन गई है।
- बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता की कमी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इसे और जटिल बना देती है।
9. सुरक्षा और हिंसा:
- बच्चों को शारीरिक, मानसिक, और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और उनके विकास में रुकावट डालता है।
- इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से बच्चों को ऑनलाइन शोषण और साइबर अपराधों का सामना भी करना पड़ रहा है।
10. सड़क दुर्घटनाएँ और शारीरिक सुरक्षा:
- भारत में सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों का शिकार होना आम बात है। बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
भारत की बाल कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनाएँ:
भारत में बच्चों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये योजनाएँ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देती हैं। निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ बाल कल्याण से संबंधित हैं:
1. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RCH):
- उद्देश्य: यह कार्यक्रम बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य, टीकाकरण, और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कार्य करता है।
- कार्य: इसमें बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पोषण संबंधी जानकारी और मातृ-शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है।
2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति भेदभाव को कम करना और उनकी शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- कार्य: बालिकाओं के लिंग अनुपात में सुधार, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, और उनके अधिकारों की रक्षा करना।
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है, ताकि उनका स्वास्थ्य और पोषण बेहतर हो सके।
- कार्य: महिलाओं को गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान स्वस्थ रखने के लिए 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
4. मिड-डे मील योजना:
- उद्देश्य: बच्चों को स्कूलों में गर्म भोजन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना है।
- कार्य: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक खाना प्रदान करना ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके।
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):
- उद्देश्य: बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना।
- कार्य: आयोग बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण, और भेदभाव को रोकने के लिए काम करता है और उनकी सुरक्षा के लिए योजनाएँ तैयार करता है।
6. पोषण अभियान (Poshan Abhiyaan):
- उद्देश्य: यह अभियान कुपोषण से प्रभावित बच्चों, महिलाओं और किशोरों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए शुरू किया गया था।
- कार्य: इसके तहत बच्चों को पोषण का सही ज्ञान और आहार प्रदान किया जाता है, और कुपोषण को समाप्त करने के उपाय किए जाते हैं।
7. राजीव गांधी शिक्षा मिशन (Sarva Shiksha Abhiyan):
- उद्देश्य: सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना।
- कार्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का स्तर बढ़ाना और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में।
8. बाल श्रम निषेध योजना:
- उद्देश्य: बच्चों को काम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
- कार्य: यह योजना बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने के लिए काम करती है, और बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है।
9. नैतिक शिक्षा और बाल सुरक्षा योजना:
- उद्देश्य: बच्चों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना।
- कार्य: बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, और उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना।
10. जन्म से मृत्यु तक स्वास्थ्य देखभाल योजना (National Health Mission):
- उद्देश्य: मातृ-शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और बच्चों के लिए सभी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना।
- कार्य: यह योजना गर्भवती महिलाओं, बच्चों, और शिशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करती है।
11. मूलभूत बालक शिक्षा योजना (Child Labour Projects):
- उद्देश्य: बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
- कार्य: बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना और उन्हें श्रमिक के रूप में काम करने से रोकना।
12. आधार योजना:
- उद्देश्य: बच्चों के लिए आधार कार्ड से जुड़ी योजना।
- कार्य: इस योजना का उद्देश्य बच्चों को उनके जन्म के समय आधार कार्ड प्रदान करना और उनकी पहचान सुनिश्चित करना है। यह योजना सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ बच्चों को सुनिश्चित करती है।
13. मुख्यमंत्री बाल विकास योजना:
- उद्देश्य: बच्चों के समग्र विकास के लिए यह योजना लागू की गई है।
- कार्य: यह योजना बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और पोषण की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर लागू की जाती है।
आगे की राह: बच्चों के कल्याण के लिए सुधार और कार्रवाई
भारत में बच्चों के कल्याण के लिए अब तक कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और उनकी सफलता के लिए कुछ सुधार की आवश्यकता है। आने वाले समय में बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:
1. शिक्षा और कौशल विकास में सुधार:
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ानी होगी। डिजिटल शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया जाए।
- कौशल विकास: बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए नई पहल की जा सकती है, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।
2. कुपोषण से निपटने के लिए प्रभावी उपाय:
- पोषण पर ध्यान केंद्रित: कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। विशेषकर बच्चों को सही आहार और पोषण देना, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास स्वस्थ हो।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: बच्चों के लिए पोषण आधारित कार्यक्रमों को विस्तारित किया जा सकता है, जैसे मिड-डे मील योजना, और पोषण जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
3. बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करना:
- कठोर कानून और निगरानी: बाल श्रम और बाल विवाह की समस्याओं को समाप्त करने के लिए कड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों को इन मामलों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपनी होगी।
- सामाजिक जागरूकता: बाल श्रम और बाल विवाह को लेकर समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि लोग इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़े हो सकें।
4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुधार:
- स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना: बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, ताकि सभी बच्चों को टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।
- मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान: मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं ताकि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जल्दी पहचाना जा सके और उन्हें समय पर उपचार मिल सके।
5. बाल अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा:
- बाल अधिकारों की शिक्षा: बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और स्कूलों में उन्हें अधिकारों से जुड़ी शिक्षा देना बेहद जरूरी है। इससे बच्चों को खुद की सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलेगी।
- सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना: बच्चों के शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण को रोकने के लिए कानून और सुरक्षा तंत्र को और अधिक सख्त किया जा सकता है।
6. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से निपटना:
- जलवायु संकट पर कार्रवाई: जलवायु परिवर्तन से बच्चों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण अभियानों को बढ़ावा देने से बच्चों को एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा।
- जलवायु-आधारित शिक्षा: बच्चों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के बारे में शिक्षा देना और उन्हें इस दिशा में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है।
7. संवेदनशील नीति और योजनाओं का विकास:
- कुशल नीति निर्माण: बच्चों के कल्याण को लेकर नीति निर्माण में सुधार की आवश्यकता है। बच्चों के लिए समर्पित योजनाओं और नीतियों का निर्माण करना और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- विकसित देशों के मॉडल का अनुसरण: भारत को विकसित देशों के सफल बाल कल्याण मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन मॉडल्स को अपने देश की स्थिति के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए।
8. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार:
- आर्थिक सुरक्षा: बालक की भलाई के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बालिका सुरक्षा योजनाओं, किशोर स्वास्थ्य योजनाओं, और गरीब परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है।
- वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन: गरीब और पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों पर विचार किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
आगे की राह में बच्चों के समग्र विकास और कल्याण के लिए हमें सरकार, समाज और निजी क्षेत्र के सहयोग से ठोस और स्थायी समाधान तलाशने होंगे। केवल नीतिगत प्रयास ही नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। यदि बच्चों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य देना है, तो हमें इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा।
UNICEF (United Nations Children’s Fund) के बारे में मुख्य तथ्य:
- स्थापना और इतिहास:
- UNICEF की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य युद्ध के बाद बच्चों की सहायता और उनके कल्याण के लिए काम करना था। शुरुआत में इसे United Nations International Children’s Emergency Fund के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे केवल UNICEF कहा गया।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है।
- उद्देश्य:
- UNICEF का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों की मदद करना है, खासकर उन बच्चों की जो युद्ध, कुपोषण, गरीबी, और अन्य संकटों से प्रभावित हैं।
- यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और समग्र कल्याण में सुधार लाने के लिए काम करता है।
- कार्य और गतिविधियाँ:
- स्वास्थ्य और पोषण: UNICEF बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कार्य करता है।
- शिक्षा: UNICEF शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की स्थापना, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है।
- बाल अधिकार: बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण से बचाने के लिए UNICEF विभिन्न देशों में कार्य करता है।
- आपातकालीन सहायता: यह संगठन प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, और अन्य आपातकालीन स्थितियों में प्रभावित बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करता है।
- विश्व स्तर पर प्रभाव:
- UNICEF का कार्य 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है।
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा है और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन (CRC) पर काम करता है।
- मुख्य योजनाएँ और अभियान:
- UNICEF “Child Friendly Cities Initiative”, “Schools for Africa”, “End Violence Against Children” जैसी विभिन्न योजनाओं और अभियानों को चलाता है।
- यह स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, और कल्याण के क्षेत्रों में कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करता है।
- UNICEF के वित्तीय स्रोत:
- UNICEF को सरकारी दान, निजी दान और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त होता है।
- इसका बजट 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक होता है, जिसमें से अधिकांश राशि विकासशील देशों में बच्चों के कल्याण पर खर्च की जाती है।
- UNICEF और COVID-19:
- COVID-19 महामारी के दौरान, UNICEF ने वैश्विक स्तर पर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और पोषण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसने महामारी के दौरान बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाए, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया और ऑनलाइन शिक्षा के उपायों को बढ़ावा दिया।
- UNICEF के प्रमुख कार्यक्रम:
- स्वास्थ्य सेवाएं: जैसे पोलियो उन्मूलन, आहार की पूर्ति, और कुपोषण के इलाज के लिए कार्यक्रम।
- शिक्षा: बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण और शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- आपातकालीन सहायता: युद्ध, भूकंप, बाढ़, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बच्चों को तत्काल सहायता।
- विश्व में प्रमुख साझेदार:
- UNICEF का विभिन्न देशों की सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), निजी क्षेत्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों जैसे WHO (World Health Organization) और UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) के साथ भी मिलकर काम करता है।
- UNICEF का प्रमुख नारा:
- UNICEF का प्रमुख नारा है “For Every Child” यानी हर बच्चे के लिए। यह नारा UNICEF के उद्देश्यों और मिशन को व्यक्त करता है, जिसमें हर बच्चे के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करना है।
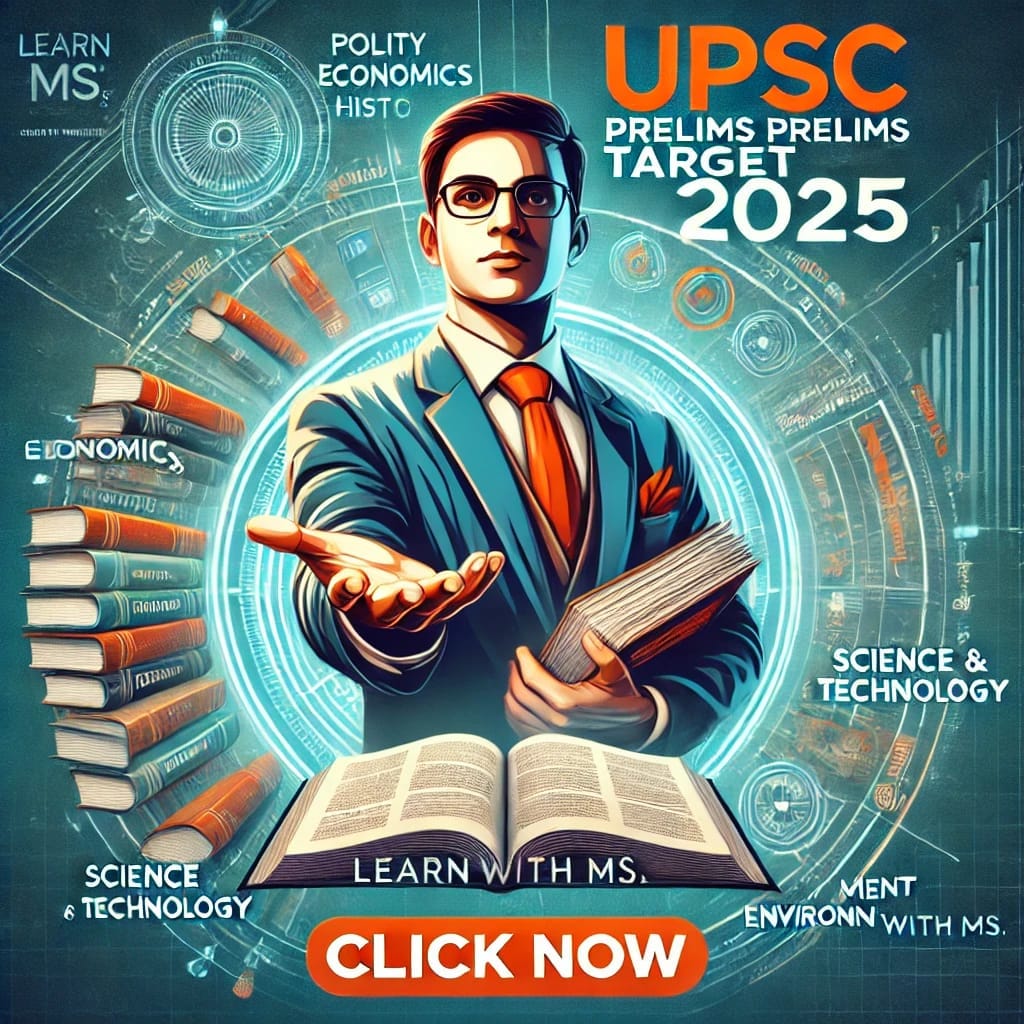
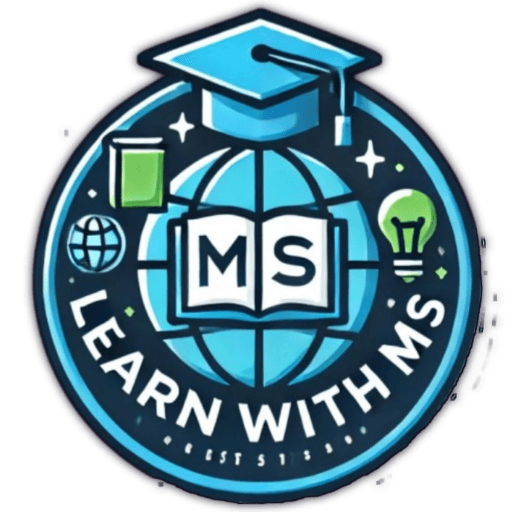

Leave a Reply