DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI FOR UPSC IAS – Prelims And Mains Examination 2025 | 05 FEBRUARY 2025 – UPSC PRELIMS POINTER Fact Based Current Affairs.
DAILY Current Affairs Analysis For UPSC Pre And Mains Examination
Daily Archiveकपास उत्पादन में सुधार हेतु पाँच वर्षीय मिशन ( Five Year Mission to Improve Cotton Production )
कपास उत्पादन में सुधार हेतु पाँच वर्षीय मिशन:
परिचय
केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय कपास खेती की उत्पादकता और सतत विकास में सुधार लाने तथा अतिरिक्त लंबा रेशा (Extra-Long Staple – ELS) कपास को बढ़ावा देने के लिए एक पाँच वर्षीय मिशन की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य भारतीय कपास किसानों की आय बढ़ाना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करना और कपास उत्पादन को टिकाऊ बनाना है। इस विश्लेषण में हम भारत में कपास उत्पादन की वर्तमान स्थिति, इस मिशन की आवश्यकता, इसकी संभावित चुनौतियाँ, और आगे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
भारत में कपास उत्पादन: वर्तमान स्थिति
1. भारत में कपास की खेती
- भारत कपास उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है, लेकिन उत्पादकता के मामले में यह कई देशों से पीछे है।
- महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं।
- भारतीय कपास का प्रमुख उपयोग वस्त्र उद्योग और निर्यात में होता है।
2. अतिरिक्त लंबा रेशा (ELS) कपास का महत्व
- ELS कपास की गुणवत्ता बेहतर होती है और इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र, प्रीमियम सूती कपड़े और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है।
- भारत में ELS कपास की मांग अधिक है, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण हमें इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है।
- यदि ELS कपास का उत्पादन बढ़ाया जाए, तो आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
3. वर्तमान चुनौतियाँ
- पारंपरिक खेती पद्धतियों के कारण उत्पादकता कम है।
- कपास की फसल कीट और रोगों से अधिक प्रभावित होती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है।
- सिंचाई की समस्या के कारण कई क्षेत्रों में कपास उत्पादन अस्थिर बना रहता है।
- नवीनतम तकनीकों और अनुसंधान की कमी से भारत का कपास उत्पादन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाया है।
पाँच वर्षीय कपास सुधार मिशन की आवश्यकता और उद्देश्य
1. इस मिशन की आवश्यकता क्यों है?
- भारतीय कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों की जरूरत है।
- ELS कपास उत्पादन को प्रोत्साहित कर भारत को आयात पर निर्भरता कम करनी होगी।
- किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें नए बाजारों से जोड़ने की आवश्यकता है।
- कपास की खेती को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और अधिक सतत (sustainable) बनाना जरूरी है।
2. मिशन के मुख्य उद्देश्य
✅ कपास उत्पादकता में सुधार – नई तकनीकों, बेहतर बीज और आधुनिक खेती पद्धतियों को अपनाना।
✅ ELS कपास के उत्पादन को बढ़ावा – भारत में अधिक ELS कपास उगाकर आयात पर निर्भरता घटाना।
✅ जलवायु-स्मार्ट खेती को प्रोत्साहन – कपास उत्पादन को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना।
✅ किसानों के लिए समर्थन और प्रशिक्षण – उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक और कीट नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देना।
✅ कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा – वस्त्र उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाला भारतीय कपास उपलब्ध कराना।
मिशन के तहत संभावित रणनीतियाँ
1. आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग
- कपास की संशोधित और उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों को विकसित करना।
- ड्रिप सिंचाई और संवहनीय जल प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना।
- कीट और बीमारियों के नियंत्रण के लिए जैविक और एकीकृत कृषि विधियों का उपयोग।
2. अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा
- कृषि अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से नए बीज और प्रौद्योगिकी विकसित करना।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ाना।
3. वित्तीय सहायता और नीति समर्थन
- किसानों को कृषि ऋण और अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देना।
- बीमा योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीति स्पष्ट करना।
4. निर्यात को बढ़ावा
- भारत को ELS कपास उत्पादन में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
- कपास के निर्यात को सुगम बनाने के लिए उत्पादन श्रृंखला को व्यवस्थित करना।
संभावित चुनौतियाँ और समाधान
1. जलवायु परिवर्तन और जल संकट
चुनौती – कपास की खेती जल पर निर्भर है, और बदलते मौसम से उत्पादन प्रभावित होता है।
समाधान – माइक्रो-सिंचाई प्रणाली (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देना और जल-संवर्धन तकनीकों का उपयोग।
2. कीट और रोगों का खतरा
चुनौती – गुलाबी सुंडी और अन्य कीटों के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
समाधान – जैविक कीटनाशकों और प्रतिरोधी बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
3. किसानों में जागरूकता की कमी
चुनौती – कई किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों से खेती कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता कम होती है।
समाधान – किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृषि हेल्पलाइन का निर्माण।
4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा
चुनौती – भारतीय कपास की गुणवत्ता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मिस्र जैसे देशों के मुकाबले कम मानी जाती है।
समाधान – बेहतर गुणवत्ता के बीजों और वैज्ञानिक प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग कर गुणवत्ता सुधार।
आगे की राह
- सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी – कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों और शोध संस्थानों को शामिल करना।
- डिजिटल और स्मार्ट कृषि को बढ़ावा – सेंसर-आधारित खेती और कृषि ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग।
- कृषि निर्यात नीति को मजबूत बनाना – भारत को कपास निर्यात में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस नीतियाँ लागू करना।
- कृषकों के लिए वित्तीय सहायता और स्थायी बाजार – किसानों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना और सरकारी खरीद नीति को मजबूत करना।
निष्कर्ष
पाँच वर्षीय कपास सुधार मिशन भारतीय कपास किसानों और वस्त्र उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। यदि सरकार सही नीति बनाकर इसे लागू करती है, तो न केवल कपास उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि भारत ELS कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। यह पहल कपास आधारित उद्योगों को भी मजबूती देगी, जिससे भारत का वैश्विक वस्त्र बाजार में दबदबा बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
बिहार में “मखाना बोर्ड” की स्थापना : Establishment of “Makhana Board” in Bihar:
बिहार में “मखाना बोर्ड” की स्थापना:
परिचय
केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की कि बिहार में “मखाना बोर्ड” की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य मखाना (फॉक्स नट) की खेती और विपणन को बढ़ावा देना है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और मखाना उद्योग के समग्र विकास में सहायक होगी। इस विश्लेषण में हम मखाना उद्योग की वर्तमान स्थिति, मखाना बोर्ड की भूमिका, संभावित चुनौतियाँ और आगे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
मखाना: एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद
1. मखाना का परिचय
- मखाना (फॉक्स नट) एक जलीय फसल है, जो मुख्यतः तालाबों और जलाशयों में उगाई जाती है।
- यह पोषण से भरपूर होता है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुरता होती है।
- भारत में इसका उपयोग स्नैक्स, मिठाइयों और आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है।
2. भारत में मखाना उत्पादन
- भारत विश्व में मखाना उत्पादन में अग्रणी है और इसका 90% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है।
- अन्य राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मखाने की खेती की जाती है।
- बिहार में दरभंगा, मिथिला, कटिहार, सुपौल, और पूर्णिया मखाना उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं।
3. मखाना की आर्थिक और पोषणीय महत्ता
- आर्थिक महत्त्व: मखाना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जो उन्हें अच्छा मुनाफा दिला सकती है।
- पोषणीय महत्त्व: इसमें उच्च प्रोटीन, कम वसा, और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिससे यह सेहतमंद स्नैक के रूप में लोकप्रिय है।
- निर्यात की संभावना: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मखाने की बढ़ती माँग को देखते हुए भारत के पास निर्यात की अपार संभावनाएँ हैं।
मखाना बोर्ड की आवश्यकता और भूमिका
1. मखाना बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता
- मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।
- विपणन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है।
- पारंपरिक खेती पद्धतियाँ होने के कारण उत्पादकता कम है।
- जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों की कमी से उत्पादन प्रभावित होता है।
2. मखाना बोर्ड की मुख्य भूमिकाएँ
(i) मखाना की खेती में सुधार
- आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
- किसानों को उन्नत बीज और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- जल प्रबंधन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाना।
(ii) विपणन और ब्रांडिंग
- मखाना के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मखाने को ब्रांडेड उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करना।
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बनाना।
(iii) प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
- मखाना प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में सहायता प्रदान करना।
- औद्योगिक स्तर पर मखाने के विभिन्न उत्पादों (मखाना फ्लेक्स, मखाना पाउडर, मखाना स्नैक्स) के विकास को बढ़ावा देना।
(iv) निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
- मखाना उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान देना।
- भारतीय मखाना को वैश्विक बाजारों में प्रचारित करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाना।
- अन्य मखाना उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई व्यापारिक रणनीतियाँ विकसित करना।
मखाना उद्योग के समक्ष संभावित चुनौतियाँ
1. जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियाँ
- मखाना जल में उगाया जाता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन, बाढ़, और सूखे जैसी समस्याएँ इसके उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं।
- जलाशयों की उचित सफाई और प्रबंधन की कमी से उत्पादन में गिरावट हो सकती है।
2. विपणन और मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याएँ
- किसानों को बिचौलियों के कारण उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।
- संगठित विपणन प्रणाली का अभाव है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाई होती है।
3. प्रसंस्करण और भंडारण की समस्या
- आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के कारण उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- भंडारण सुविधाएँ सीमित होने के कारण किसानों को जल्द ही अपनी उपज बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें कम कीमत मिलती है।
4. निर्यात संबंधी कठिनाइयाँ
- भारतीय मखाना अभी भी बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं किया जा रहा है।
- गुणवत्ता मानकों और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण की कमी के कारण वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है।
मखाना बोर्ड के माध्यम से आगे की संभावनाएँ
- तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा – आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से मखाना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
- MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी – किसानों को उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए MSP लागू किया जा सकता है।
- लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज – भंडारण और परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ विकसित करनी होंगी।
- निर्यात संवर्धन – भारतीय मखाना को वैश्विक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत कर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ाया जा सकता है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी – मखाना उद्योग में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को शामिल कर नवाचार और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
निष्कर्ष
बिहार में “मखाना बोर्ड” की स्थापना एक दूरदर्शी कदम है, जो किसानों की आय बढ़ाने और मखाना उद्योग को संगठित करने में सहायक होगा। यह पहल उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक स्तर पर मखाना उत्पादन में अग्रणी बना सकती है। हालाँकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार, किसान संगठनों, और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय आवश्यक होगा। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएँ, तो मखाना उद्योग भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
भारत में ऊर्जा रूपांतरण और ऊर्जा सुरक्षा ( Energy Conversion and Energy Security in India )
भारत में ऊर्जा रूपांतरण और ऊर्जा सुरक्षा: संतुलन की आवश्यकता
भारत एक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, जिसकी ऊर्जा मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में, ऊर्जा रूपांतरण (एनर्जी ट्रांज़िशन) और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (जैसे कोयला) और नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है ताकि पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा सके।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कोयले की भूमिका
भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए, कोयला अभी भी एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। देश में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा कोयले से आता है। भारी उद्योग, इस्पात उत्पादन, सीमेंट उद्योग और थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला आवश्यक बना हुआ है। हालाँकि, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के कारण कोयले के उपयोग को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।
हाल ही में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में स्पष्ट किया गया है कि भारत के ऊर्जा रूपांतरण के बावजूद कोयले की महत्ता बनी रहेगी। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं:
- सस्ते और सुलभ ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला: भारत के पास विशाल कोयला भंडार हैं, जिससे यह अन्य ईंधनों की तुलना में किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा विकल्प बना हुआ है।
- औद्योगिक विकास के लिए अपरिहार्य: इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन जैसे उद्योगों को अभी भी बड़े पैमाने पर कोयले की आवश्यकता होती है।
- बेस-लोड पावर सप्लाई का प्रमुख स्रोत: नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के बावजूद, स्थिर ऊर्जा आपूर्ति के लिए कोयले का योगदान महत्वपूर्ण है।
कोयला आधारित ऊर्जा में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत
हालांकि भारत 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, लेकिन कोयले पर पूर्ण निर्भरता को समाप्त करना निकट भविष्य में संभव नहीं है। इस कारण सरकार कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन को अधिक स्वच्छ और प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:
- उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (AUSC) तकनीक – यह नई तकनीक कोयले से बिजली उत्पादन को अधिक कुशल बनाएगी और उत्सर्जन को कम करेगी।
- कोयला गैसीकरण और तरलकरण – इन तकनीकों से कोयले का स्वच्छ और प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा।
- कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) – यह तकनीक कोयला संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को पकड़कर उसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करेगी।
- पर्यावरण अनुकूल खनन नीतियाँ – कोयला खदानों को अधिक सतत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए नई नीतियाँ अपनाई जा रही हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की रणनीति
भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है:
1. सौर ऊर्जा का विस्तार
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
- सौर ऊर्जा पार्कों का विकास राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में किया जा रहा है।
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा।
2. पवन ऊर्जा में बढ़ोतरी
- भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में।
- सरकार ऑफशोर विंड फार्म्स विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे स्थायी ऊर्जा आपूर्ति संभव होगी।
3. जलविद्युत और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ
- भारत पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता को दूर किया जा सके।
- जलविद्युत परियोजनाएँ ऊर्जा भंडारण और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होंगी।
4. परमाणु ऊर्जा का विस्तार
- भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और उन्नत परमाणु संयंत्रों के विकास पर ध्यान दे रहा है।
- परमाणु ऊर्जा एक स्थिर और कम-कार्बन ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है।
आवश्यक खनिज मिशन और ऊर्जा रूपांतरण
भारत सरकार ने हाल ही में आवश्यक खनिज मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। यह मिशन विशेष रूप से बैटरी भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक होगा।
ऊर्जा रूपांतरण और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा:
- रोजगार के नए अवसर – नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश से नए रोजगार सृजित होंगे।
- विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा – स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से पेट्रोलियम और कोयले के आयात पर निर्भरता घटेगी।
- औद्योगिक क्रांति – ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास से भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनेगा।
केंद्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु कौन-सी घोषणाएँ की गई हैं?
केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: इस योजना के तहत, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए 6,250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनियमितता को प्रबंधित करने के लिए, सरकार पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे बिजली ग्रिड में स्थिरता सुनिश्चित होगी।
- परमाणु ऊर्जा विकास: बजट में भारत स्मॉल रिएक्टर और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की योजना है, जिसमें नई परमाणु प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन शामिल है।
- आवश्यक खनिज मिशन: इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और अधिग्रहण को बढ़ावा देना है, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक होंगे।
- उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (AUSC) थर्मल पावर प्लांट: एनटीपीसी और बीएचईएल के सहयोग से, 800 मेगावाट का AUSC तकनीक वाला थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो उच्च दक्षता वाली बिजली उत्पादन सुनिश्चित करेगा।
- पारंपरिक उद्योगों के लिए समर्थन: 60 पारंपरिक लघु और कुटीर उद्योगों के समूहों में ऊर्जा ऑडिट और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी स्थिरता बढ़ेगी।
- जलवायु अनुकूलन और शमन के प्रयास: सरकार 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु सहने वाली फसल किस्मों को जारी करेगी और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: 400 जिलों में खरीफ फसल का डिजिटल सर्वेक्षण और 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन को रजिस्ट्री में शामिल करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण: जलवायु अनुकूलन और शमन के प्रयासों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक नया वर्गीकरण प्रणाली विकसित की जाएगी।
- बाढ़ प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता: बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए प्रावधान शामिल हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।
ऊर्जा रूपांतरण की चुनौतियाँ
हालांकि ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:
- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की उच्च लागत – सौर और पवन ऊर्जा की लागत में गिरावट आ रही है, लेकिन अभी भी प्रारंभिक निवेश काफी अधिक है।
- ऊर्जा भंडारण की समस्या – नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनियमितता के कारण ऊर्जा भंडारण की जरूरत बढ़ रही है, जिसके लिए अत्याधुनिक बैटरी तकनीक की आवश्यकता होगी।
- बेस-लोड पावर सप्लाई में चुनौतियाँ – नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पूरी तरह से अपनाने से पहले, कोयला और परमाणु ऊर्जा जैसे स्थिर स्रोतों को संतुलित करना आवश्यक होगा।
निष्कर्ष
भारत ऊर्जा रूपांतरण और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाए हुए है। सरकार कोयले की भूमिका को बनाए रखते हुए इसे अधिक स्वच्छ और कुशल बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं नवीकरणीय ऊर्जा को भी गति दी जा रही है।
इन प्रयासों से न केवल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। अगले कुछ वर्षों में, भारत का ऊर्जा क्षेत्र एक बड़े बदलाव से गुजरेगा, जिससे यह वैश्विक स्तर पर स्वच्छ और सतत ऊर्जा नेतृत्व की ओर अग्रसर होगा।
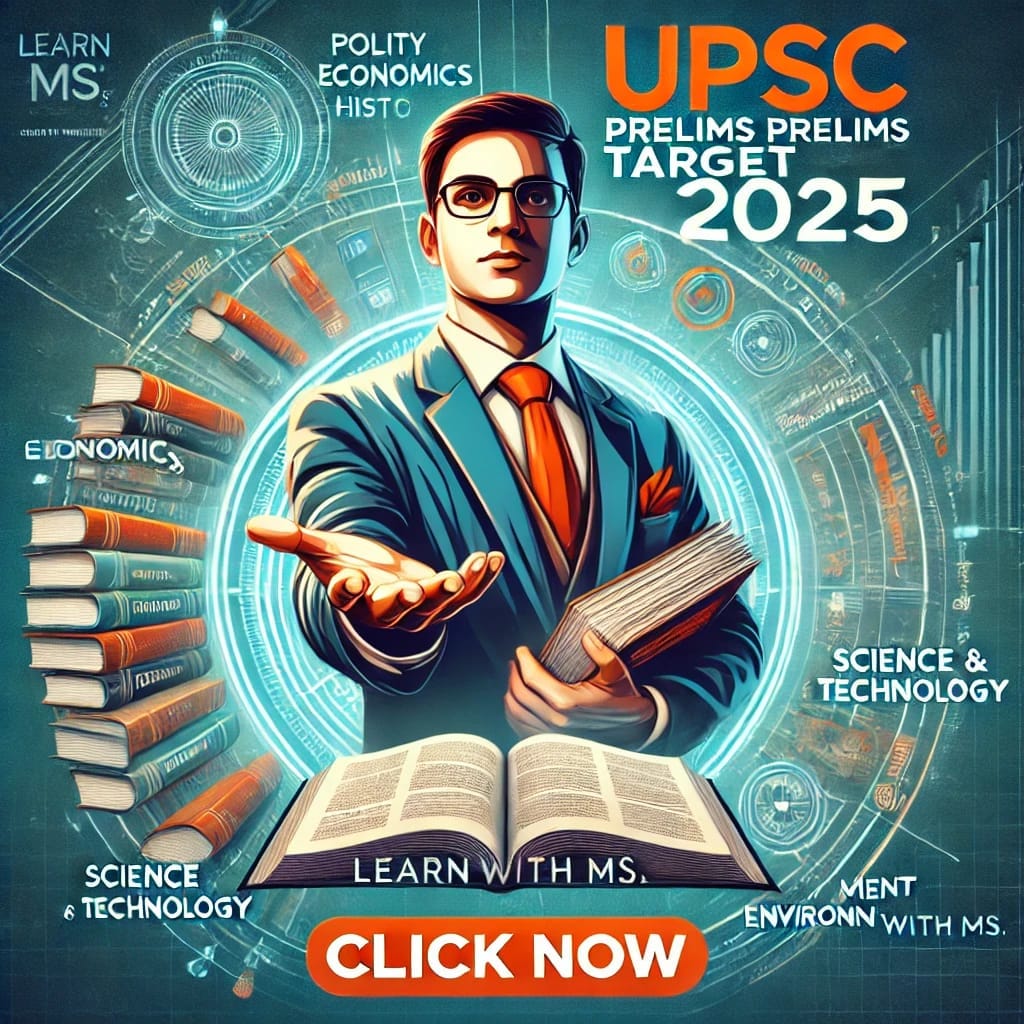
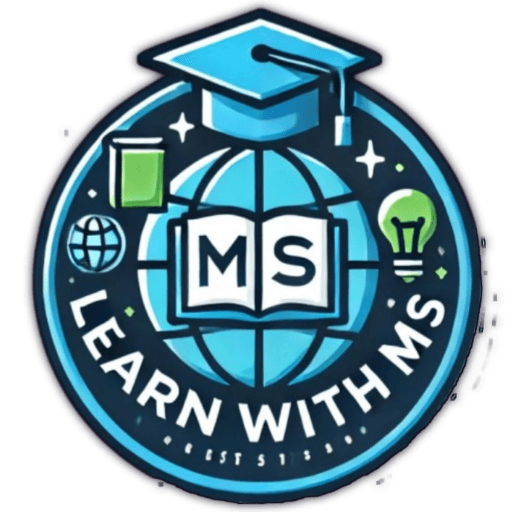
Leave a Reply